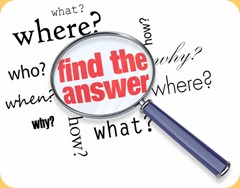“चीज़” की व्युत्पत्ति के जन्मसूत्र इंडो-ईरानी भाषा परिवार के प्रश्नवाची सर्वनाम से जुड़े हैं। सृष्ठि में जो कुछ भी दृश्यमान है, सब “पदार्थ” की श्रेणी में आता है। वैशैषिक दर्शन में विश्व को छह पदार्थों (द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय) में समेट दिया गया है। मनुष्य का मूल स्वभाव है अस्तित्व के प्रति जिज्ञासु होना। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जागृत विश्व में अस्तित्व के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने के लिए छह प्रकार के ककार हैं। हिन्दी में इन्हें प्रश्नवाची सर्वनाम अर्थात क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन कहा जाता है। इन्हें ककार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें “क” वर्ण या ध्वनि है। इसी तरह अंग्रेजी में फाईव डब्ल्यू और वन एच में भी यही बात हैं। गौरतलब है कि हमारे यहाँ "क" की महिमा है तो अंग्रेजी में "डब्ल्यू" की। इनमें रिश्तेदारी है, जिसकी चर्चा आगे। संस्कृत के “क” (कः) वर्ण में जिज्ञासा का भाव महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि “चीज़” के मूल में भी इसी ‘क’ की माया है। हिन्दी की अनेक बोलियों में जानने के लिए, प्रश्नवाचक “की/ki” (की?) शब्द बोला जाता है। अभिप्राय “क्या” से होता है। “की” में “क्यों” का भाव भी है। इंडो-ईरानी भाषा परिवार में इस “की” का रूपान्तर “ची” में भी होता है। लोक बोली में मुख-सुख के आधार पर “क्यों” के “चों” या “च्यों” जैसे रूप भी सुनने को मिलते हैं। तुतलाने वाले भी “क्यों” की एवज में “च्यों” का उच्चार करते हैं।
बहरहाल “की/ki” का प्रयोग “क्या” अथवा “कौन” के लिए होता है, यह स्थापित सत्य है। प्रश्नवाची सर्वनाम “किस” पर विचार करते हुए भाषाविज्ञानी भोलानाथ तिवारी संस्कृत के “कस्य” शब्द के आदिरूप “किस्य” की कल्पना करते हैं। इसमें संस्कृत के “किम्” का पुरानी फ़ारसी में “चिम्” रूप बतलाते हैं। इसी तरह डॉ फ्रिट्ज़ रोज़ेन भी फ़ारसी में कौन के लिए “की ki” और क्या के लिए “ची chi” शब्द में अंतर्संबंध बताते हैं। बात को और स्पष्ट करने के लिए एक और सर्वनाम की मिसाल देखते हैं। हिन्दी का अनिश्चयवाची सर्वनाम है “कुछ”। हिन्दी की विभिन्न बोलियों में इसके “कुच्छो, कछू, किछु” जैसे रूप भी मिलते हैं। इसका प्रयोग निर्जीव पदार्थों के अस्तित्व को उजागर करने के लिए होता है। उदयनारायण तिवारी समेत अनेक विद्वानों ने कुछ की व्युत्पत्ति किं-चिद् से मानी है जिसका हिन्दी रूप किंचित् है। पदार्थ के अस्तित्व का यही भाव “की/ki” के फ़ारसी रूपान्तर “ची” में भी देखने को मिलता है और इसी वज़ह से वस्तु या पदार्थ के अर्थ में ही प्रश्नवाची सर्वनाम “ची” का रूपान्तर “चीज़” हो गया। अलबत्ता पदार्थ के प्रति कुछ में जो तुच्छता का भाव है, वैसा “चीज़” में नहीं है। “चीज़” में जब तुच्छता प्रकट की जाती है तो उसके आगे विलोमार्थक “ना” उपसर्ग लगाकर “नाचीज़” शब्द बनाया जाता है अर्थात जो तुच्छ हो। तुच्छ वही है जो हीन है, क्षीण है या महीन है। जाहिर है चीज़ में महत्व निहित है। यह भी कि किं-चिद् से अगर “कुछ” बनता है तो “ची”(की) से “चीज़” बनना तार्किक है।
चीज़ में ज्यादातर वैशिष्ट्य, महत्वपूर्ण जैसी अर्थवत्ता है। कोई खास वस्तु, कीमती पदार्थ, मालमत्ता, माल-असबाब, सम्पत्ति, खास आदमी वगैरह चीज़ के दायरे में आते हैं। मराठी में भी “चीज़” और “चीज़बस्त” शब्द का अर्थ कीमती पदार्थ, खास बात या कोई पदार्थ, टुकड़ा, पीस piece ही है। जेटी मोल्सवर्थ अपने मराठी कोश में चीज़ का अर्थ स्पष्ट करते हुए मिसाल देते हैं कि गायन जैसी कोई चीज़ नहीं ( गायना सारखी दुसरी चीज नाहीं) ज़ाहिर है यहाँ चीज़ का अभिप्राय कला से है। यानी पदार्थ की श्रेणी में गुण भी शामिल है। इसके विपरीत मराठी में कभी कभी तुच्छता का भाव प्रकट करने के लिए भी चीज़ का प्रयोग होता है जैसे- इस लड़के ने तो मेरी मेहनत की “चीज़” कर दी (ह्या पोराने माझ्या श्रमाचे चीज केले) यहाँ आशय मेहनत पर पानी फेरने से ही है। खानोलकर और सरमोकदम के मुताबिक बखानने योग्य बात, सराहने योग्य बात भी “चीज़” हैं मसलन किसी कविता की पंक्ति, कोई उक्ति या श्लोक आदि। संगीत घरानों में पुरानी घरानेदार बंदिश को चीज़ कहने की रिवायत रही है जैसे-राग दरबारी की एक चीज़ पेश है।
इंडो-ईरानी परिवार का “चीज़” शब्द अंग्रेजी में भी गया और वहाँ इसका रूप हुआ Cheese. पश्चिमी भाषाविज्ञानियों के अनुसार अंग्रेजी का चीज़ Cheese भी उर्दू-फ़ारसी के चीज़ से ही गया है जिसका अर्थ है पदार्थ, कुछ आदि। भाषा विज्ञानियों के मुताबिक पुरानी फ़ारसी में “किस-की” जैसे शब्दों का अर्थ वही था जो संस्कृत के “कस्य” या “किस्य” का था। यहाँ ध्यान रखा जाना चाहिए कि बाद के दौर में किस-की के “चिस-ची” जैसे रूप बने होंगे तभी “ची” से “चीज़” जैसे सूप सामने आए। “किस” में भी “कौन” का ही भाव है। एटिमऑनलाइन के मुताबिक इसका रिश्ता प्रोटो इंडो-यूरोपीय धातु kwo- से ही जिससे ही अंग्रेजी का “हू who” (कौन) बना है। गौर करें संस्कृत में भी प्रश्नवाचक सर्वनाम “क/ka” से शुरू होते है और भारोपीय भाषाओं में भी जैसे अवेस्ता में को, रूसी में क्तो, लिथुआनी में कस, लैटिन में क्वी, क्वे, क्वोद, स्लोवानी में कुतो ( संस्कृत के कुतः से साम्यता देखें) आदि। बात यहाँ भी प्रश्नवाची सर्वनाम से ही जुड़ रही है। अंग्रेजी के चीज़ की अर्थवत्ता भी महत्वपूर्ण है। औपनिवैशिक काल के शुरुआती दौर में इसकी अर्थवत्ता में तुच्छता का भाव था मगर बाद में असली माल, बड़ी बात या ऐसी कोई भी चीज़ जो खास हो, के अर्थ में चीज़ का मुहावरेदार प्रयोग होने लगा। हॉब्सन जॉब्सन के कोश से इसका पता चलता है।
अब आते हैं चीज़बस्त पर। दरअसल यह सामासिक पद है और “चीज़” तथा “बस्त” से मिल कर बना है। फ़ारसी में “बस्त” में भी वस्तु का ही भाव है। वस्तु का एक रूपान्तर बत्तू भी होता है। चीज़ भी पदार्थ है और वस्तु भी पदार्थ है। समान अर्थ वाले शब्दों के मेल से बने सामासिक पद अकसर लोकभाषा में मुखसुख के आधार पर बनते हैं जैसे सामान-सुमान। भारोपीय भाषाओं में “व” का रूपान्तर “ब” में होना आम बात है सो संस्कृत की वस्तु फ़ारसी में “बस्त” हो जाती है। वस्तु बना है “वस्” धातु से। संस्कृत की वस् धातु में रहने का भाव है। गौरतलब है कि वस्तु यानी पदार्थ के रूप में “वस्” धातु का अर्थ अवस्थिति, उपस्थिति या मौजूदगी से है। भाव अस्तित्व का ही है। वासः यानी मकान के अर्थ में निवास, आवास जैसे शब्द भी इसी मूल से आ रहे हैं। परिधान के अर्थ में कपड़ों के लिए वस्त्र शब्द भी इसी मूल से निकला है। वस् अर्थात जिसमें वास किया जाए। यह दिलचस्प है कि काया जिस आवरण में निवास करती है, उसे वस्त्र कहा जाए। वस् धातु का अर्थ होता है ढकना, रहना, डटे रहना आदि। यही नहीं, गाँव देहात में आज भी घरों के संकुल या मौहल्ले के लिए बास या बासा (गिरधर जी का बासा) शब्द काफी प्रचलित है। वस् से ही बना है वसति जिससे निवास या रहने का भाव है। हिन्दी का बस्ती शब्द इससे ही बना है। इस तरह वस्तु का अर्थ हुआ कोई चल या अचल पदार्थ।
कुछ लोग इस बस्त को बंदोबस्त या बस्तोबंद वाले बस्त से जोड़ कर देखते हैं। इस दूसरे बस्त का अर्थ होता है बांध कर रखा हुआ या बांधा हुआ। संस्कृत का “बद्ध” अवेस्ता में बस्तः हुआ जिसका मतलब हुआ जिसे बांधकर, जमा कर, तह कर या गठरी बांधकर रखा गया हो। इसी से बना फारसी-उर्दू में बस्ता यानी स्कूल बैग या पोथी-पोटली। पुराने जमाने में विद्याध्ययन के लिए छात्रों को दूर दूर तक जाना पड़ता था और वे घर से कई तरह का सामान साथ ले जाया करते थे। तब सफर भी पैदल या घोड़ों पर ही तय किया जाता था जाहिर है सामान को सुरक्षित रखने के लिए उसे बेहद विश्वसनीय तरीके से बांधकर या जकड़ कर रखा जाता था। यह क्रिया पहले बद्ध कहलाई फिर इससे बस्तः शब्द बना। इसमें गठरी बैडिंग या पुलंदे का भाव था। बाद में बस्ता के रूप में स्कूलबैग के अर्थ में सिमट कर रह गया।
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
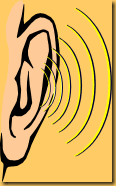
 ‘अकनि’ और ‘ऐकणे’ की व्युत्पत्ति कल्पित ‘अक्’ धातु की बजाय ‘कर्ण’ में ही निहित है। प्रोटो भारोपीय भाषाओं के मूल स्रोतों की दिशा में महान काम करने वाले जूलियस पकोर्नी जैसे ख्यात भाषा शास्त्री का ध्यान इस ओर नहीं गया होगा, यह बात मानना मुश्किल है।
‘अकनि’ और ‘ऐकणे’ की व्युत्पत्ति कल्पित ‘अक्’ धातु की बजाय ‘कर्ण’ में ही निहित है। प्रोटो भारोपीय भाषाओं के मूल स्रोतों की दिशा में महान काम करने वाले जूलियस पकोर्नी जैसे ख्यात भाषा शास्त्री का ध्यान इस ओर नहीं गया होगा, यह बात मानना मुश्किल है। 

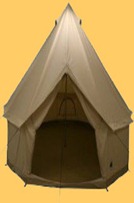 ... तम्बू को खड़ा करने में रस्सी और डण्डे की बड़ी भूमिका है। इसी तरह मवेशियों को बांध कर रखने में भी रस्सी एक ख़ास ज़रिया है। तम्बू ही बद्दुओं का आश्रय था। तम्बू में ही गृहस्थी की अर्थवत्ता समायी है अर्थात दुनियादारी की सभी वस्तुएँ...
... तम्बू को खड़ा करने में रस्सी और डण्डे की बड़ी भूमिका है। इसी तरह मवेशियों को बांध कर रखने में भी रस्सी एक ख़ास ज़रिया है। तम्बू ही बद्दुओं का आश्रय था। तम्बू में ही गृहस्थी की अर्थवत्ता समायी है अर्थात दुनियादारी की सभी वस्तुएँ...