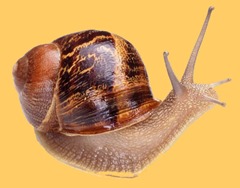फ़ारसी का कमीना
‘कम’ शब्द की तरह ही ‘कमीन’ शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में भी हिन्दी कोश ज्यादा जानकारी नहीं देते हैं । अलबत्ता यह स्पष्ट है कि हिन्दी में आज गाली की तरह मशहूर ‘कमीना’ शब्द फ़ारसी मूल के ‘कमीनः’ (कमीनह्) से बना है । संस्कृत-फारसी का विसर्ग हिन्दी में स्वर हो जात है । सवाल यह है कि ‘कमीन’ शब्द कहाँ से आया है ? मोटे तौर पर तो ‘कमीन’ और ‘कमीना’ एक ही जान पड़ते हैं मगर ‘कमीना’ जहाँ सौ फ़ीसद फ़ारसी शब्द है, वहीं ‘कमीन’ शब्द का रिश्ता एकाध जगह फ़ारसी से और कुछ जगह हिन्दी से बताया गया है । हिन्दी, उर्दू, फ़ारसी के कई कोशों में तो ‘कमीन’ शब्द दर्ज़ तक नहीं हुआ है । शायद इसीलिए कि ‘कमीन’ को ‘कमीना’ का पर्याय मान लिया गया । मद्दाह के उर्दू-हिन्दी कोश ‘कमीन’ शब्द है ही नहीं और फ़ैलन के कोश में ‘कमीन’ शब्द को तो हिन्दी का बताया गया है मगर उसकी व्युत्पत्ति फ़ारसी ‘कमीनः’ से बताई गई है । ‘कमीन’ का अर्थ फ़ैलन नीच जात बताते हैं और ‘कमीना’ का अर्थ टहलुआ, चाकर, सेवक, नौकर, दास आदि । फैलन ‘कार-कमीन’ और ‘कमीन-कंडु’ शब्दों का उल्लेख भी करते हैं ।
कम्मी से कमीन
‘कमीन’ शब्द प्राचीन भारतीय समाज की जजमानी प्रथा के सन्दर्भ में सामने आता है और इसीलिए मेरे विचार में हिन्दी के ‘कमीन’ और ‘कमीना’ दो अलग अलग शब्द है, दोनों की अलग अलग अर्थवत्ता है और दोनों के जन्मसन्दर्भ भी पृथक है । ‘कमीना’ बना है फ़ारसी के ‘कमीनः’ से जिसके मूल में ‘थोड़ा’, ‘कुछ’, ‘न्यून’ के अर्थवाला फ़ारसी का ‘कम’ शब्द है । इसका रिश्ता पुरानी फ़ारसी और अवेस्ता के ‘कम्ना’ शब्द से है । दूसरी ओर ‘कमीन’ शब्द के मूल में संस्कृत का ‘कर्म’ शब्द है । पाली, अपभ्रंश में ‘कर्म’ का ‘कम्म’ रूप होता है । हिन्दी के विभिन्न रूपों में ‘कार्य’ के अर्थ में प्रचलित ‘काम’ शब्द इसी ‘कम्म’ का अगला रूप है । जिस तरह हिन्दी का ‘काम’ शब्द पाली , अपभ्रंश के ‘कम्म’ का रूपान्तर है उसी तरह पाली के ‘कम्मी’, ‘कम्मिक’ ( पाली हिन्दी कोश, भदन्त आनन्द कौसल्यायन ) का रूपान्तर है हिन्दी का ‘कमीन’ शब्द जिसका आशय है कार्मिक, कर्मी, करने वाला , मज़दूर, श्रमिक आदि । प्रचलित तौर पर वे जातियाँ जो सेवाएँ लेती हैं उन्हें ‘जजमान’ कहते हैं और वे जातियाँ जो सेवाएँ प्रदान करती हैं, उन्हें ‘कमीन’ कहते हैं । सो काम करने वाले ‘कम्मी’ कहलाए । अब यहाँ ‘कमीन’ नीच व्यक्ति नहीं है बल्कि इसका अर्थ है ‘कार्मिक – कर्मकार’ । शोषण का दायरा जब व्यापक हुआ तब निम्नवर्गीय सेवाओं और गौण कृषिकर्म करने वाले तबकों को ‘कम्मी’ कहा जाने लगा । बाद के दौर में तो ब्राह्मणों के सेवाकर्म को छोड़ कर शेष सभी सेवाएँ गौण कर्म समझी जाने लगीं मसलन, खेत-मजूरी, हस्तशिल्प, कुम्हारी, लुहारी जैसे काम, घास छीलना, बाँस छीलना जैसे काम करने वाले समुदाय ‘कमीन’ जाति कहलाने लगे ।
कम्मकर से कमेरा
इन्हीं अर्थों में पाली में ‘कम्मकर’, ‘कम्मकार’ जैसे शब्द भी हैं जिनसे हिन्दी का ‘कमेरा’ शब्द बना है । ‘कमेरा’ यानी मज़दूरी करने वाला । ‘कम्मी’ यानी कमाने वाला । चाकर, सहायक, छोटे-मोटे काम करने वाला ही ‘कमेरा’ है । फैलन के कोश में जो ‘कार-कमीन’ है वह दरअसल ‘कारकम्मी’ ही है । इसी तरह हिन्दी – उर्दू कोशों में ‘कमीनकंडु’ शब्द मिलता है जिसका अर्थ पुराने ज़माने में तीर तैयार करना था । गौरतलब है संस्कृत में ‘काण्ड’ शब्द बाँस की गाँठ को कहते हैं । बाँस छील कर तीर बनाने वाला ‘काण्डपाल’ कहलाता है । इससे ही बना है ‘कण्डु’ या ‘कडु’ शब्द । जाहिर यह कर्म से जुड़ा नाम है इसलिए इसके साथ जुड़े ‘कमीन’ शब्द का पूर्वरूप ‘कम्मी’ ही तार्किक है । इसी तरह मुहावरेदार भाषा में ‘कम्मीं-कमीन’ शब्दयुग्म का प्रयोग भी होता है । यहाँ ‘कम्मीं’ और ‘कमीन’ दोनों का अर्थ अलग अलग है । यहाँ ‘कम्मीं’ का आशय छोटी जात या ओछा काम करने वाले से है जबकि कमीन में फ़ारसी वाले ‘कमीना’ ( नीच, धूर्त, क्षुद्र, लफंगा, बदमाश ) का आशय निकलता है । ख्यात लेखक यशपाल ने मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास में कमीन का अर्थ “ बेगार, कठिन परिश्रम और अप्रिय काम करने वाले ” बताया है । कम्मी और कम्मा के अवशेष हमें आज भी अपने आसपास मिलते हैं । कमीना में कमीन की तलाश करने वाले ज़रा पहचानें निकम्मा और निकम्मी जैसे शब्दों को । जिसके पास काम नहीं है वह निकम्मा, जो व्यस्था काम न करे वह निकम्मी । ये बेहद प्रचलित शब्द हैं । मूल भाव है कर्म का । लोगों को काम करना चाहिए । कम्मी यानी कामगार । बाद में यह हीनकर्म के अर्थ में रूढ़ हो गया ।
कम्मी यानी प्रजा
‘कमीन’ और ‘कमीना’ शब्द भाव सादृष्य और अर्थ सादृष्य के चलते आपस में कुछ इस तरह घुलमिल गए कि ये एक मूल से जन्मे जुड़वाँ शब्द नज़र आने लगे । ध्यान देने की बात है कि यजमानी प्रथा से जुड़े ‘कम्मी’ शब्द में कामगार के भाव के साथ प्रजा का भाव भी है । अब यह कहने की ज़रूरत नहीं कि संरक्षण और शोषण भी एक चीज़ के दो आयाम हैं । किसी के संरक्षण में जाते ही शोषण का आरम्भ होता है । मगर मूलतः शोषण की शुरुआत पुचकारने से होती है । अतः यह नहीं माना जा सकता कि अपने शुरुआती दौर में ही यजमानी प्रथा का ‘कमीन’ शब्द सचमुच गाली का दर्ज़ा रखता था । समूची प्रजा, रियाया के लिए गाली समान शब्द का प्रचलन भला किसी भी काल की सत्ता-व्यवस्था में क्योंकर सम्भव होगा ? निश्चित ही फ़ारसी ने जब हिन्दुस्तान की धरती पर पैर रखा तब ‘कमीनः’ का ‘कमीना’ रूप भी विकसित हुआ । इसमे निहित कमतरता के दास्यभाव की अवनति हुई । बाद में ओछापन, नीचता, तुच्छता जैसे भावों का स्पष्ट विकास हुआ । शब्दों अर्थावनति के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं । बोलचाल की भाषा में फ़ारसी के कमीन का चलन बढ़ा और जनमानस में सदियों से प्रचलित पाली का ‘कम्मीं’ भी ‘कमीन’ बन गया । इस तरह हिन्दी की ज़मीन पर मेरे विचार से दो ‘कमीन’ विराजमान हैं । एक फ़ारसी से आया हुआ और दूसरा फ़ारसी के प्रभाव में बना हुआ ।
शायर कमीना, आशिक कमीना
रही बात फ़ारसी के ‘कमीनः’ की तो न्यून, हीन, छोटा, क्षुद्र, ओछा आदि के अर्थ वाला कम ही इसके मूल में है । ‘कमीनः’ शब्द अपने मूल रूप में यह शब्द गाली या अपशब्द नहीं था, मगर बाद में हो गया । ‘कमीन’ का आशय था अपने पालक की तुलना में हीन, क्षीण, दीन आदि । साधक प्रायः खुद को ईश्वर की तुलना में दीन, हीन, कमजोर ही मानता है । मध्यकालीन सधुक्कड़ी भाषा के कवियों नें प्रायः इसी अर्थ में खुद को ‘कमीन’ कहा है । शायरी भी मूलतः सूफ़ीयाना काव्य परम्परा से ही जन्मी है । शायरों ने खुद को हक़ीर माना । इश्को-आशिकी की उनकी रचनाएँ दरअसल आध्यात्मिक अनुभूतियाँ ही हैं जिनमें माशूक का प्रयोग ब्रह्म के रूप में हुआ है । शायरों ने भी इसीलिए खुद को हक़ीर, गुलाम, फ़क़ीर और ‘कमीन’ तक कहा है, सो इसी भावना से । शायर भी कमीना, आशिक भी कमीना । इसका अर्थ लफंगा, बदमाश तो कतई नहीं, बल्कि विनम्रतावश खुद को कमतर मानने का भाव ही है यहा है । पर मेरा मानना है कि जातिवाचक कमीन शब्द का व्युत्पत्तिक आधार चाहे फ़ारसी के कमीन से न जुड़ता हो मगर जातिवाची संज्ञा के तौर पर ‘कमीन’ शब्द का प्रयोग मुस्लिम दौर में ही बढ़ा है । ‘कमीन’ में निहित ओछेपन के भाव का विस्तार ही हीन जाति के अर्थ में हुआ । बाद में इसमें नीच, अधम, धूर्त जैसे भाव समा गए और इस तरह ‘कमीन’ और ‘कमीना’ एक हो गए । अगली कड़ी- किसी कंपेश को जानते हैं आप ?
सम्बन्धित आलेख- 1.ये भी पाखण्डी और वो भी पाखण्डी 2.‘अहदी’ यानी आलसी की ओहदेदारी 3.मदरसे में बैठा मदारी…[संत-8] 4.गुरुघंटाल लवगुरु, हो जा शुरु.... 5.समझदार से बुद्धू की रिश्तेदारी
 ब चपन से युवावस्था तक अपन मालवी-उमठवाड़ी परिवेश वाले राजगढ़-ब्यावरा में पले-बढ़े हैं। मालवी में जब हाड़ौती का तड़का लगता है तो उमठवाड़ी बनती है। हालाँकि राजगढ़-ब्यावरा मूल रूप से मध्यप्रदेश के मालवांचल में ही आता है फिर भी इस इलाके की स्थानीय पहचान उमठवाड़ के नाम से भी है। बहरहाल अक्सर महिलाओं के आपसी संवादों में ‘दारी’ और ‘दरी’ इन शब्दों का अलग अलग ढंग से इस्तेमाल सुना करते थे। ‘दरी’ में जहाँ अपनत्व और साख्य-भाव है वहीं ‘दारी’ में उपेक्षा और भर्त्सना का दंश होता है। ‘दरी’ का प्रयोग देखें- “रेबा दे दरी” अर्थात रहने दो सखि। “आओ नी दरी” यानी सखि, आओ न। “अरी दरी, असाँ कसाँ हो सके” मतलब ऐसा कैसे हो सकता है सखि! इसके ठीक विपरीत ‘दारी’ शब्द का प्रयोग बतौर उपेक्षा या गाली के तौर पर किया जाता है जैसे- “दारी, घणो मिजाज दिखावे”, भाव है- इसकी अकड़ तो देखो!
ब चपन से युवावस्था तक अपन मालवी-उमठवाड़ी परिवेश वाले राजगढ़-ब्यावरा में पले-बढ़े हैं। मालवी में जब हाड़ौती का तड़का लगता है तो उमठवाड़ी बनती है। हालाँकि राजगढ़-ब्यावरा मूल रूप से मध्यप्रदेश के मालवांचल में ही आता है फिर भी इस इलाके की स्थानीय पहचान उमठवाड़ के नाम से भी है। बहरहाल अक्सर महिलाओं के आपसी संवादों में ‘दारी’ और ‘दरी’ इन शब्दों का अलग अलग ढंग से इस्तेमाल सुना करते थे। ‘दरी’ में जहाँ अपनत्व और साख्य-भाव है वहीं ‘दारी’ में उपेक्षा और भर्त्सना का दंश होता है। ‘दरी’ का प्रयोग देखें- “रेबा दे दरी” अर्थात रहने दो सखि। “आओ नी दरी” यानी सखि, आओ न। “अरी दरी, असाँ कसाँ हो सके” मतलब ऐसा कैसे हो सकता है सखि! इसके ठीक विपरीत ‘दारी’ शब्द का प्रयोग बतौर उपेक्षा या गाली के तौर पर किया जाता है जैसे- “दारी, घणो मिजाज दिखावे”, भाव है- इसकी अकड़ तो देखो!