
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |

| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |

| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
 प्रचलित हुए तो उन्हें ज़ार फ़ानूस कहा जाने लगा होगा। मगर इस विचार का प्रमाण मुझे नहीं मिला। हालाँकि अंग्रेजी का जार शब्द अरबी से आया है। दरअसल लटकते हुए कंदील फ्रांसीसी सैनिक असबाब का एक ख़ास हिस्सा थे। मैदानों, जंगलों, रेगिस्तानों में जब सैनिक पड़ाव होते थे, तब पेड़ों पर या पेड़नुमा जंगलों पर लालटेनों को लटका कर बड़े क्षेत्र को प्रकाशित किया जाता था। दरअसल पुरानी फ्रैंच में candeltreow शब्द दीपाधार के लिए प्रयुक्त होता था। बाद में अंग्रेजी में इससे कैंडल-ट्री कहा जाने लगा। मुझे लगता है इस कैंडल-ट्री की तर्ज पर ही फ़ानूस के साथ ट्री के अर्थ में झाड़ शब्द लगाकर हिन्दी में झाड़-फ़ानूस पद प्रचलित हुआ होगा।
प्रचलित हुए तो उन्हें ज़ार फ़ानूस कहा जाने लगा होगा। मगर इस विचार का प्रमाण मुझे नहीं मिला। हालाँकि अंग्रेजी का जार शब्द अरबी से आया है। दरअसल लटकते हुए कंदील फ्रांसीसी सैनिक असबाब का एक ख़ास हिस्सा थे। मैदानों, जंगलों, रेगिस्तानों में जब सैनिक पड़ाव होते थे, तब पेड़ों पर या पेड़नुमा जंगलों पर लालटेनों को लटका कर बड़े क्षेत्र को प्रकाशित किया जाता था। दरअसल पुरानी फ्रैंच में candeltreow शब्द दीपाधार के लिए प्रयुक्त होता था। बाद में अंग्रेजी में इससे कैंडल-ट्री कहा जाने लगा। मुझे लगता है इस कैंडल-ट्री की तर्ज पर ही फ़ानूस के साथ ट्री के अर्थ में झाड़ शब्द लगाकर हिन्दी में झाड़-फ़ानूस पद प्रचलित हुआ होगा। | ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
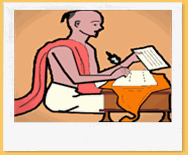
 तारीख़ लिखना या ब्याज की गणना करना, मिती पूजना या मिती उगना का अर्थ है हुंडी की अवधि पूरी होना, भुगतान का दिन आना। अब आते हैं बदी और सुदी पर।
तारीख़ लिखना या ब्याज की गणना करना, मिती पूजना या मिती उगना का अर्थ है हुंडी की अवधि पूरी होना, भुगतान का दिन आना। अब आते हैं बदी और सुदी पर। ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
 पहली शुभकामना दूर-देहात के बच्चों को। वे बच्चे जो सचिन और सानिया जैसे बनना चाहते हैं। दम है इसलिए ख्वाहिश है। पर हालत की पूछिए मत और हालात जाकर देखिए। न मैदान, न कोच। न सडक़, न बिजली। कोई बात नहीं। रात के बाद सुबह होती है। सपने देखो। बड़े सपने। वी केन डू एवरीथिंग। पता है ये किसकी शुभकामना है? माननीय सुरेश कलमाड़ी की। तालियां...
पहली शुभकामना दूर-देहात के बच्चों को। वे बच्चे जो सचिन और सानिया जैसे बनना चाहते हैं। दम है इसलिए ख्वाहिश है। पर हालत की पूछिए मत और हालात जाकर देखिए। न मैदान, न कोच। न सडक़, न बिजली। कोई बात नहीं। रात के बाद सुबह होती है। सपने देखो। बड़े सपने। वी केन डू एवरीथिंग। पता है ये किसकी शुभकामना है? माननीय सुरेश कलमाड़ी की। तालियां... | ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
प्रस्तुतकर्ता
अजित वडनेरकर
10
कमेंट्स
पर
2:07 AM
![]() लेबल:
इधर उधर,
उत्सव
लेबल:
इधर उधर,
उत्सव
 इसका रूप हुआ मास्क यानी मुखौटा। मध्यकाल में मसखरा शब्द ने मेकअप और कास्मैटिक की दुनिया में प्रवेश पाया और इसका रूपांतर मस्कारा mascara में हो गया जिसके तहत मेकअप करते समय महिलाएं काले रंग के आईलाईनर से अपनी भौहों और पलकों को नुकीला और गहरा बनाती हैं। आवारगी, बेचारगी, दीवानगी की तर्ज पर मस्खरः में ‘अगी’ प्रत्यय लगने से अरब,फारसी में बनता है मस्खरगी यानी मसख़रापन या ठिठोलेबाजी। मगर इसके विपरीत इसमें ‘शुदा’ प्रत्यय लगने से बन जाता है विकृत, रूपांतरित आदि।
इसका रूप हुआ मास्क यानी मुखौटा। मध्यकाल में मसखरा शब्द ने मेकअप और कास्मैटिक की दुनिया में प्रवेश पाया और इसका रूपांतर मस्कारा mascara में हो गया जिसके तहत मेकअप करते समय महिलाएं काले रंग के आईलाईनर से अपनी भौहों और पलकों को नुकीला और गहरा बनाती हैं। आवारगी, बेचारगी, दीवानगी की तर्ज पर मस्खरः में ‘अगी’ प्रत्यय लगने से अरब,फारसी में बनता है मस्खरगी यानी मसख़रापन या ठिठोलेबाजी। मगर इसके विपरीत इसमें ‘शुदा’ प्रत्यय लगने से बन जाता है विकृत, रूपांतरित आदि। | ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |

| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
प्रस्तुतकर्ता
अजित वडनेरकर
10
कमेंट्स
पर
1:51 AM
![]() लेबल:
उत्सव,
सम्बोधन,
संस्कृति
लेबल:
उत्सव,
सम्बोधन,
संस्कृति
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
प्रस्तुतकर्ता
अजित वडनेरकर
21
कमेंट्स
पर
3:18 AM
![]() लेबल:
god and saints,
उत्सव,
संस्कृति
लेबल:
god and saints,
उत्सव,
संस्कृति
 कि टैक्स यानी कर का संबंध कार्य करने से है, कर यानी हाथों से है। भारतीय संस्कृति में हाथ अर्थात "कर" को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है कि उसे सभी प्रकार के कर्मों का आवास कहा गया है। प्रातःकाल उठते ही स्व हस्त दर्शनम् के आध्यात्मिक अर्थ है। सुख-समृद्धि और कल्याण – मंगल के चिह्न भारतीय मनीषा हथेलियों में देखती है- कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वतीम्। करमूले स्थिता काली प्रभाते कर दर्शनम्।। अर्थात हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती, मूल में काली का निवास होने से सुबह हथेलियों को देखना शुभ होता है।
कि टैक्स यानी कर का संबंध कार्य करने से है, कर यानी हाथों से है। भारतीय संस्कृति में हाथ अर्थात "कर" को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है कि उसे सभी प्रकार के कर्मों का आवास कहा गया है। प्रातःकाल उठते ही स्व हस्त दर्शनम् के आध्यात्मिक अर्थ है। सुख-समृद्धि और कल्याण – मंगल के चिह्न भारतीय मनीषा हथेलियों में देखती है- कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वतीम्। करमूले स्थिता काली प्रभाते कर दर्शनम्।। अर्थात हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती, मूल में काली का निवास होने से सुबह हथेलियों को देखना शुभ होता है।  गौर करें शरीर से बाहर निकलती दो भुजाएं वृद्धि का ही प्रतीक हैं। यूं भी भुजाओं का लम्बा होना शुभकारी माना जाता है। शास्त्रों में असमान भुजाओं वाले व्यक्ति को चोर कहा गया है। छोटी भुजाओवाला व्यक्ति दास होता है। घुटनों तक लम्बी भुजाओं वाला व्यक्ति दैवीय और राजसी गुणों से सम्पन्न होता है। ईश्वर को आजानुभुज कहा गया है क्योंकि उनकी भुजाएं लम्बी होती हैं।
गौर करें शरीर से बाहर निकलती दो भुजाएं वृद्धि का ही प्रतीक हैं। यूं भी भुजाओं का लम्बा होना शुभकारी माना जाता है। शास्त्रों में असमान भुजाओं वाले व्यक्ति को चोर कहा गया है। छोटी भुजाओवाला व्यक्ति दास होता है। घुटनों तक लम्बी भुजाओं वाला व्यक्ति दैवीय और राजसी गुणों से सम्पन्न होता है। ईश्वर को आजानुभुज कहा गया है क्योंकि उनकी भुजाएं लम्बी होती हैं।  संक्षिप्त रूप ताली हुआ। हाथ के लिए संस्कृत में हस्त शब्द है। हथेली बना है हस्त+तालिकः = हथेली से। हस्त यानी हाथ और तालिकः यानी खुला पंजा जिसकी सतह नजर आती है। यही हाथ का तल या सतह है जो भूमि पर टिकती है। हाथ का महत्व अपना हाथ जगन्नाथ जैसी कहावत में भी नजर आता है। कर शब्द में विशालता का भाव भी है जो मूलतः वृद्धि अर्थात समृद्धि से जुड़ा है। गौर करें शरीर से बाहर निकलती दो भुजाएं वृद्धि का ही प्रतीक हैं। यूं भी भुजाओं का लम्बा होना शुभकारी माना जाता है। शास्त्रों में असमान भुजाओं वाले व्यक्ति को चोर कहा गया है। छोटी भुजाओवाला व्यक्ति दास होता है। घुटनों तक लम्बी भुजाओं वाला व्यक्ति दैवीय और राजसी गुणों से सम्पन्न होता है। ईश्वर को आजानुभुज कहा गया है क्योंकि उनकी भुजाएं लम्बी होती हैं। इसी अर्थ में अपना हाथ, जगन्नाथ जैसी लोकोक्ति को भी समझना चाहिए।
संक्षिप्त रूप ताली हुआ। हाथ के लिए संस्कृत में हस्त शब्द है। हथेली बना है हस्त+तालिकः = हथेली से। हस्त यानी हाथ और तालिकः यानी खुला पंजा जिसकी सतह नजर आती है। यही हाथ का तल या सतह है जो भूमि पर टिकती है। हाथ का महत्व अपना हाथ जगन्नाथ जैसी कहावत में भी नजर आता है। कर शब्द में विशालता का भाव भी है जो मूलतः वृद्धि अर्थात समृद्धि से जुड़ा है। गौर करें शरीर से बाहर निकलती दो भुजाएं वृद्धि का ही प्रतीक हैं। यूं भी भुजाओं का लम्बा होना शुभकारी माना जाता है। शास्त्रों में असमान भुजाओं वाले व्यक्ति को चोर कहा गया है। छोटी भुजाओवाला व्यक्ति दास होता है। घुटनों तक लम्बी भुजाओं वाला व्यक्ति दैवीय और राजसी गुणों से सम्पन्न होता है। ईश्वर को आजानुभुज कहा गया है क्योंकि उनकी भुजाएं लम्बी होती हैं। इसी अर्थ में अपना हाथ, जगन्नाथ जैसी लोकोक्ति को भी समझना चाहिए। | ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
 देशभर में दशनामियों की कुल 52 मढ़ियां हैं जो शंकराचार्यों की चारों पीठों द्वारा नियंत्रित हैं। सर्वाधिक 27 मठिकाएं गिरि दशनामियों की है
देशभर में दशनामियों की कुल 52 मढ़ियां हैं जो शंकराचार्यों की चारों पीठों द्वारा नियंत्रित हैं। सर्वाधिक 27 मठिकाएं गिरि दशनामियों की है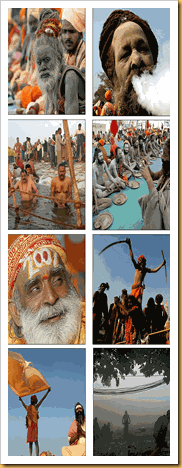 सन्यासी पोथी, चोला का मोह छोड़ कर थोड़े समय के लिए शस्त्रविद्या सीखते थे बल्कि आमजन को भी इन अखाड़ों के जरिये आत्मरक्षा (प्रकारांतर से धर्मरक्षा ) के लिए सामरिक कलाए सिखाते थे। इस तरह अखाड़ों के जरिये धर्मरक्षक सेना का एक स्वरूप बनता चला गया। हिन्दूधर्म को इस्लाम की आंधी से बचाने के लिए सिख पंथ एक सामरिक संगठन के तौर पर ही सामने आया था। इसके महान गुरुओं ने अध्यात्म की रोशनी में लोगों को धर्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाने की प्रेरणा दी। अखाड़ों का यह स्वरूप प्रायः हर धर्म-सम्प्रदाय में रहा है। दुनियाभर के धार्मिक आंदोलनों के साथ अखाड़ा अर्थात आत्मरक्षा से जुड़ी तकनीक को ध्यान-प्राणायाम से जोड़कर अपनाया गया। हर धार्मिक सम्प्रदाय के साथ शस्त्रधारी रहे हैं और धर्म या पंथ अथवा मठ पर आए खतरों का सामना इन्होंने किया है। बौद्ध धर्म चीन तक पहुंचाने का श्रेय पांचवीं सदी के जिन आचार्य बोधिधर्म को दिया जाता है उन्हें ही चीन की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट शैलियों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। अहिंसक धर्म के आचार्य ने मूलतः ध्यान केन्द्रित करने की तकनीक के तौर पर इस कला को जन्म दिया जिसे बाद में आत्मरक्षा की कला के तौर पर मान्यता दे दी गई। गौरतलब है कि ध्यान ही जापान पहुंच कर ज़ेन हुआ। मध्यकाल मे चारों पीठों से जुड़ी दर्जनों पीठिकाएं सामने आई जिन्हें मठिका कहा गया। इसका देशज रूप मढ़ी प्रसिद्ध हुआ। देशभर में दशनामियों की ऐसी कुल 52 मढ़ियां हैं जो चारों पीठों द्वारा नियंत्रित हैं। इनमें सर्वाधिक 27 मठिकाएं गिरि दशनामियों की है, 16 मठिकाओं में पुरी नामधारी सन्यासी काबिज है, 4 मढ़ियों में भारती नामधारी दशनामियों का वर्चस्व है और एक मढ़ी लामाओं की है। साधुओं में दंडी और गोसाईं दो प्रमुख भेद भी हैं। तीर्थ, आश्रम, भारती और सरस्वती दशनामी दंडधर साधुओं की श्रेणी में आते है जबकि बाकी गोसाईं कहलाते हैं।
सन्यासी पोथी, चोला का मोह छोड़ कर थोड़े समय के लिए शस्त्रविद्या सीखते थे बल्कि आमजन को भी इन अखाड़ों के जरिये आत्मरक्षा (प्रकारांतर से धर्मरक्षा ) के लिए सामरिक कलाए सिखाते थे। इस तरह अखाड़ों के जरिये धर्मरक्षक सेना का एक स्वरूप बनता चला गया। हिन्दूधर्म को इस्लाम की आंधी से बचाने के लिए सिख पंथ एक सामरिक संगठन के तौर पर ही सामने आया था। इसके महान गुरुओं ने अध्यात्म की रोशनी में लोगों को धर्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाने की प्रेरणा दी। अखाड़ों का यह स्वरूप प्रायः हर धर्म-सम्प्रदाय में रहा है। दुनियाभर के धार्मिक आंदोलनों के साथ अखाड़ा अर्थात आत्मरक्षा से जुड़ी तकनीक को ध्यान-प्राणायाम से जोड़कर अपनाया गया। हर धार्मिक सम्प्रदाय के साथ शस्त्रधारी रहे हैं और धर्म या पंथ अथवा मठ पर आए खतरों का सामना इन्होंने किया है। बौद्ध धर्म चीन तक पहुंचाने का श्रेय पांचवीं सदी के जिन आचार्य बोधिधर्म को दिया जाता है उन्हें ही चीन की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट शैलियों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। अहिंसक धर्म के आचार्य ने मूलतः ध्यान केन्द्रित करने की तकनीक के तौर पर इस कला को जन्म दिया जिसे बाद में आत्मरक्षा की कला के तौर पर मान्यता दे दी गई। गौरतलब है कि ध्यान ही जापान पहुंच कर ज़ेन हुआ। मध्यकाल मे चारों पीठों से जुड़ी दर्जनों पीठिकाएं सामने आई जिन्हें मठिका कहा गया। इसका देशज रूप मढ़ी प्रसिद्ध हुआ। देशभर में दशनामियों की ऐसी कुल 52 मढ़ियां हैं जो चारों पीठों द्वारा नियंत्रित हैं। इनमें सर्वाधिक 27 मठिकाएं गिरि दशनामियों की है, 16 मठिकाओं में पुरी नामधारी सन्यासी काबिज है, 4 मढ़ियों में भारती नामधारी दशनामियों का वर्चस्व है और एक मढ़ी लामाओं की है। साधुओं में दंडी और गोसाईं दो प्रमुख भेद भी हैं। तीर्थ, आश्रम, भारती और सरस्वती दशनामी दंडधर साधुओं की श्रेणी में आते है जबकि बाकी गोसाईं कहलाते हैं।  इसका प्रयोग भी होता है। आज की ही तरह प्राचीनकाल में भी शासन की तरफ से एक निर्धारित स्थान पर जुआ खिलाने का प्रबंध रहता था जिसे अक्षवाटः कहते थे। यह बना है दो शब्दों अक्ष+वाटः से मिलकर। अक्षः के कई अर्थ है जिनमें एक अर्थ है चौसर या चौपड़, अथवा उसके पासे। वाटः का अर्थ होता है घिरा हुआ स्थान। यह बना है संस्कृत धातु वट् से जिसके तहत घेरना, गोलाकार करना आदि भाव आते हैं। इससे ही बना है उद्यान के अर्थ में वाटिका जैसा शब्द। चौपड़ या चौरस जगह के लिए बने वाड़ा जैसे शब्द के पीछे भी यही वट् धातु झांक रही है। इसी तरह वाटः का एक रूप बाड़ा भी हुआ जिसका अर्थ भी घिरा हुआ स्थान है। वर्ण विस्तार से कही कहीं इसे बागड़ भी बोला जाता है। इस तरह देखा जाए तो अक्षवाटः का अर्थ हुआ जहां पर पांसों का खेल खेला जाए । जाहिर है कि पांसों से खेला जानेवाला खेल जुआ ही है सो अक्षवाटः का अर्थ हुआ द्यूतगृह अर्थात जुआघर। अखाड़ा शब्द कुछ यूं बना - अक्षवाटः > अक्खाडअ > अक्खाडा > अखाड़ा। द्यूतगृह जब अखाड़ा कहलाने लगा और खेल के दांव-पेंच से ज्यादा महत्व हार-जीत का हो गया तो नियम भी बदलने लगे। अब दांव पर रकम ही नहीं , कुछ भी लगाया जाने लगा । महाभारत का द्यूत-प्रसंग सबको पता है। इसी तरह अखाड़े में वे सब शारीरिक क्रियाएं भी आ गईं जिन्हें क्रीड़ा की संज्ञा दी जा सकती थी और जिन पर दांव लगाया जा सकता था। जाहिर है प्रभावशाली लोगों के बीच आन-बान की नकली लड़ाई के लिए कुश्ती इनमें सबसे खास शगल था , सो घीरे धीरे कुश्ती का बाड़ा अखाड़ा कहलाने लगा और जुआघर को अखाड़ा कहने का चलन खत्म हो गया। अब तो व्यायामशाला को भी अखाड़ा कहते हैं और साधु-सन्यासियों के मठ या रुकने के स्थान को भी अखाड़ा कहा जाता है। कहां जुआ खेलने की जगह और कहां साधु-सन्यासियों की संगत ! [समाप्त]
इसका प्रयोग भी होता है। आज की ही तरह प्राचीनकाल में भी शासन की तरफ से एक निर्धारित स्थान पर जुआ खिलाने का प्रबंध रहता था जिसे अक्षवाटः कहते थे। यह बना है दो शब्दों अक्ष+वाटः से मिलकर। अक्षः के कई अर्थ है जिनमें एक अर्थ है चौसर या चौपड़, अथवा उसके पासे। वाटः का अर्थ होता है घिरा हुआ स्थान। यह बना है संस्कृत धातु वट् से जिसके तहत घेरना, गोलाकार करना आदि भाव आते हैं। इससे ही बना है उद्यान के अर्थ में वाटिका जैसा शब्द। चौपड़ या चौरस जगह के लिए बने वाड़ा जैसे शब्द के पीछे भी यही वट् धातु झांक रही है। इसी तरह वाटः का एक रूप बाड़ा भी हुआ जिसका अर्थ भी घिरा हुआ स्थान है। वर्ण विस्तार से कही कहीं इसे बागड़ भी बोला जाता है। इस तरह देखा जाए तो अक्षवाटः का अर्थ हुआ जहां पर पांसों का खेल खेला जाए । जाहिर है कि पांसों से खेला जानेवाला खेल जुआ ही है सो अक्षवाटः का अर्थ हुआ द्यूतगृह अर्थात जुआघर। अखाड़ा शब्द कुछ यूं बना - अक्षवाटः > अक्खाडअ > अक्खाडा > अखाड़ा। द्यूतगृह जब अखाड़ा कहलाने लगा और खेल के दांव-पेंच से ज्यादा महत्व हार-जीत का हो गया तो नियम भी बदलने लगे। अब दांव पर रकम ही नहीं , कुछ भी लगाया जाने लगा । महाभारत का द्यूत-प्रसंग सबको पता है। इसी तरह अखाड़े में वे सब शारीरिक क्रियाएं भी आ गईं जिन्हें क्रीड़ा की संज्ञा दी जा सकती थी और जिन पर दांव लगाया जा सकता था। जाहिर है प्रभावशाली लोगों के बीच आन-बान की नकली लड़ाई के लिए कुश्ती इनमें सबसे खास शगल था , सो घीरे धीरे कुश्ती का बाड़ा अखाड़ा कहलाने लगा और जुआघर को अखाड़ा कहने का चलन खत्म हो गया। अब तो व्यायामशाला को भी अखाड़ा कहते हैं और साधु-सन्यासियों के मठ या रुकने के स्थान को भी अखाड़ा कहा जाता है। कहां जुआ खेलने की जगह और कहां साधु-सन्यासियों की संगत ! [समाप्त]| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |

 के बाद सम्राट की सार्वभौमिकता सिद्ध हो जाती थी। विद्वानों के मुताबिक प्राचीनकाल में विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग यज्ञों का विधान था। क्षत्रिय के लिए राजसूय यज्ञ धर्म था तो ब्राह्मण के लिए अधर्म। वाजपेय यज्ञ ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए धर्म था मगर वैश्य के लिए अधर्म। क्षत्रिय यज्ञकर्ता के लिए यह यज्ञ राज्याभिषेक से लेकर सम्राट पद प्राप्ति का निमित्त था और ब्राह्मण के लिए यह पुरोहित पद का पूर्वसंस्कार था। वाज या वाजि शब्द में निहित शक्ति का प्रतीकार्थ आयुर्वेद में भी काम आया। आयुर्वेद में ओषधि के जरिए शक्तिवर्धक प्रक्रिया को वाजिकरण कहा जाता है। यहां भाव अश्व के समान शक्तिवान होने से ही है। यह स्पष्ट है कि वाजपेय अनुष्ठान करानेवाले यज्ञकर्ता ही वाजपेयी कहलाए। क्षत्रिय शासक द्वारा प्रतिष्ठा सिद्ध करने हेतु किए वाजपेय यज्ञ के बाद वह राजा या सम्राट कहलाता था और ब्राह्मण इस यज्ञ के बाद पुरोहित पद का अधिकारी होता था। दिलचस्प है यह कि इस अनुष्ठान के जरिये पुरोहित का रुतबा हासिल करनेवाले ब्राह्मणों ने अपने नाम के साथ वाजपेयी जोड़ कर इस यज्ञ को पुरोहित उपाधि की तुलना में भी अधिक महत्व दिया।
के बाद सम्राट की सार्वभौमिकता सिद्ध हो जाती थी। विद्वानों के मुताबिक प्राचीनकाल में विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग यज्ञों का विधान था। क्षत्रिय के लिए राजसूय यज्ञ धर्म था तो ब्राह्मण के लिए अधर्म। वाजपेय यज्ञ ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए धर्म था मगर वैश्य के लिए अधर्म। क्षत्रिय यज्ञकर्ता के लिए यह यज्ञ राज्याभिषेक से लेकर सम्राट पद प्राप्ति का निमित्त था और ब्राह्मण के लिए यह पुरोहित पद का पूर्वसंस्कार था। वाज या वाजि शब्द में निहित शक्ति का प्रतीकार्थ आयुर्वेद में भी काम आया। आयुर्वेद में ओषधि के जरिए शक्तिवर्धक प्रक्रिया को वाजिकरण कहा जाता है। यहां भाव अश्व के समान शक्तिवान होने से ही है। यह स्पष्ट है कि वाजपेय अनुष्ठान करानेवाले यज्ञकर्ता ही वाजपेयी कहलाए। क्षत्रिय शासक द्वारा प्रतिष्ठा सिद्ध करने हेतु किए वाजपेय यज्ञ के बाद वह राजा या सम्राट कहलाता था और ब्राह्मण इस यज्ञ के बाद पुरोहित पद का अधिकारी होता था। दिलचस्प है यह कि इस अनुष्ठान के जरिये पुरोहित का रुतबा हासिल करनेवाले ब्राह्मणों ने अपने नाम के साथ वाजपेयी जोड़ कर इस यज्ञ को पुरोहित उपाधि की तुलना में भी अधिक महत्व दिया। | ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
 Saveभोपाल में पुस्तक पाएँ- चांदना बुक हाऊस,GF-19, मानसरोवर काम्प्लेक्स, हबीबगंज स्टेशन के पास, होशंगाबाद रोड। फोन-2573061
सफ़र का पहला पड़ाव
Saveभोपाल में पुस्तक पाएँ- चांदना बुक हाऊस,GF-19, मानसरोवर काम्प्लेक्स, हबीबगंज स्टेशन के पास, होशंगाबाद रोड। फोन-2573061
सफ़र का पहला पड़ाव
 पुस्तक मंगाने के लिए लिखें-http://www.rajkamalprakashan.com/राजकमल प्रकाशन, 1-B नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
पुस्तक मंगाने के लिए लिखें-http://www.rajkamalprakashan.com/राजकमल प्रकाशन, 1-B नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

 बहुत शोधपरक, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां। हिंदी में इतनी संलग्नता के साथ ऐसा परिश्रम करने वाले विरले ही होंगे।
बहुत शोधपरक, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां। हिंदी में इतनी संलग्नता के साथ ऐसा परिश्रम करने वाले विरले ही होंगे। 'शब्दों का सफर' मुझे व्यक्तिगत रूप से हिन्दी का सबसे समृद्ध और श्रमसाध्य ब्लॉग लगता रहा है।
'शब्दों का सफर' मुझे व्यक्तिगत रूप से हिन्दी का सबसे समृद्ध और श्रमसाध्य ब्लॉग लगता रहा है।
 आप के समर्पण और लगन के लिए मेरे पास ढेर सारी प्रशंसा है और काफ़ी सारी ईर्ष्या भी।
आप के समर्पण और लगन के लिए मेरे पास ढेर सारी प्रशंसा है और काफ़ी सारी ईर्ष्या भी। सच कहूँ ,ब्लॉग-जगत का सूर और ससी ही है शब्दों का सफ़र . बधाई.... अंतर्मन से
सच कहूँ ,ब्लॉग-जगत का सूर और ससी ही है शब्दों का सफ़र . बधाई.... अंतर्मन से  लिखते रहें. यह मेरे इष्ट चिट्ठों मे से एक है क्योंकि आप काफी उपयोगी जानकारी दे रहे हैं.
लिखते रहें. यह मेरे इष्ट चिट्ठों मे से एक है क्योंकि आप काफी उपयोगी जानकारी दे रहे हैं. थोड़े में कितना कुछ कह जाते हैं आप. आपके ब्लाँग का नियमित पारायण कर रहा हूं और शब्दों की दुनिया से नया राब्ता बन रहा है.
थोड़े में कितना कुछ कह जाते हैं आप. आपके ब्लाँग का नियमित पारायण कर रहा हूं और शब्दों की दुनिया से नया राब्ता बन रहा है. आपकी मेहनत कमाल की है। आपका ये ब्लॉग प्रकाशित होने वाली सामग्री से अटा पड़ा है - आप इसे छपाइये !
आपकी मेहनत कमाल की है। आपका ये ब्लॉग प्रकाशित होने वाली सामग्री से अटा पड़ा है - आप इसे छपाइये ! मुझे सबसे उल्लेखनीय बात लगती है, पहले से ही सजीली भाषा में अभिव्यक्ति और अर्थवत्ता के अनोखे गुण का विकास। आपके ब्लॉग में रोचकता भी है और सूचनारंजन भी। मंसूर अली हाशमी
मुझे सबसे उल्लेखनीय बात लगती है, पहले से ही सजीली भाषा में अभिव्यक्ति और अर्थवत्ता के अनोखे गुण का विकास। आपके ब्लॉग में रोचकता भी है और सूचनारंजन भी। मंसूर अली हाशमी
 बेहतरीन उपलब्धि है आपका ब्लाग! मैं आपकी इस बात की तारीफ़ करता हूं और जबरदस्त जलन भी रखता हूं कि आप अपनी पोस्ट इतने अच्छे से मय समुचित फोटो ,कैसे लिख लेते हैं.
बेहतरीन उपलब्धि है आपका ब्लाग! मैं आपकी इस बात की तारीफ़ करता हूं और जबरदस्त जलन भी रखता हूं कि आप अपनी पोस्ट इतने अच्छे से मय समुचित फोटो ,कैसे लिख लेते हैं. सोमाद्रि
सोमाद्रि  इस सफर में आकर सब कुछ सरल और सहज लगने लगता है। बस, ऐसे ही बनाये रखिये. आपको शायद अंदाजा न हो कि आप कितने कितने साधुवाद के पात्र हैं.
इस सफर में आकर सब कुछ सरल और सहज लगने लगता है। बस, ऐसे ही बनाये रखिये. आपको शायद अंदाजा न हो कि आप कितने कितने साधुवाद के पात्र हैं.
 शब्दों का सफर मेरी सर्वोच्च बुकमार्क पसंद है -मैं इसे नियमित पढ़ता हूँ और आनंद विभोर होता हूँ !आपकी ये पहल हिन्दी चिट्ठाजगत मे सदैव याद रखी जायेगी.
शब्दों का सफर मेरी सर्वोच्च बुकमार्क पसंद है -मैं इसे नियमित पढ़ता हूँ और आनंद विभोर होता हूँ !आपकी ये पहल हिन्दी चिट्ठाजगत मे सदैव याद रखी जायेगी. भाषिक विकास के साथ-साथ आप शब्दों के सामाजिक योगदान और समाज में उनके स्थान का वर्णन भी बडी सुन्दरता से कर रहे हैं।आपको पढना सुखद लगता है।
भाषिक विकास के साथ-साथ आप शब्दों के सामाजिक योगदान और समाज में उनके स्थान का वर्णन भी बडी सुन्दरता से कर रहे हैं।आपको पढना सुखद लगता है। आपकी मेहनत को कैसे सराहूं। बस, लोगों के बीच आपके ब्लाग की चर्चा करता रहता हूं। आपका ढिंढोरची बन गया हूं। व्यक्तिगत रूप से तो मैं रोजाना ऋणी होता ही हूं.
आपकी मेहनत को कैसे सराहूं। बस, लोगों के बीच आपके ब्लाग की चर्चा करता रहता हूं। आपका ढिंढोरची बन गया हूं। व्यक्तिगत रूप से तो मैं रोजाना ऋणी होता ही हूं. आपकी पोस्ट पढ़ने में थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ता है. पर पढ़ने पर जो ज्ञानवर्धन होताहै,वह बहुत आनन्ददायक होता है.
आपकी पोस्ट पढ़ने में थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ता है. पर पढ़ने पर जो ज्ञानवर्धन होताहै,वह बहुत आनन्ददायक होता है. किसी हिन्दी चिट्ठे को मैं ब्लागजगत में अगर हमेशा जिन्दा देखना चाहूंगा, तो वो यही होगा-शब्दों का सफर.
किसी हिन्दी चिट्ठे को मैं ब्लागजगत में अगर हमेशा जिन्दा देखना चाहूंगा, तो वो यही होगा-शब्दों का सफर. निश्चित ही हिन्दी ब्लागिंग में आपका ब्लाग महत्वपूर्ण है. जहां भाषा विज्ञान पर मह्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध रह्ती है.
निश्चित ही हिन्दी ब्लागिंग में आपका ब्लाग महत्वपूर्ण है. जहां भाषा विज्ञान पर मह्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध रह्ती है. 
 good,innovative explanation of well known words look easy but it is an experts job.My heartly best wishes.
good,innovative explanation of well known words look easy but it is an experts job.My heartly best wishes. चयन करते हैं, जिनके अर्थ को लेकर लोकमानस में जिज्ञासा हो सकती हो। फिर वे उस शब्द की धातु, उस धातु के अर्थ और अर्थ की विविध भंगिमाओं तक पहुँचते हैं। फिर वे समानार्थी शब्दों की तलाश करते हुए विविध कोनों से उनका परीक्षण करते हैं. फिर उनकी तलाश शब्द के तद्भव रूपों तक पहुंचती है और उन तद्बवों की अर्थ-छायाओं में परिभ्रमण करती है। फिर अजित अपने भाषा-परिवार से बाहर निकलकर इतर भाषाओँ और भाषा-परिवारों में जा पहुँचते हैं। वहां उन देशों की सांस्कृतिक पृष्टभूमि में सम्बंधित शब्द का परीक्षणकर, पुनः समष्टिमूलक वैश्विक परिदृश्य का निर्माण कर देते हैं। यह सब रचनाकार की प्रतिभा और उसके अध्यवसाय के मणिकांचन योग से ही संभव हो सका है। व्युत्पत्तिविज्ञान की एक नयी और अनूठी समग्र शैली सामने आई है।
चयन करते हैं, जिनके अर्थ को लेकर लोकमानस में जिज्ञासा हो सकती हो। फिर वे उस शब्द की धातु, उस धातु के अर्थ और अर्थ की विविध भंगिमाओं तक पहुँचते हैं। फिर वे समानार्थी शब्दों की तलाश करते हुए विविध कोनों से उनका परीक्षण करते हैं. फिर उनकी तलाश शब्द के तद्भव रूपों तक पहुंचती है और उन तद्बवों की अर्थ-छायाओं में परिभ्रमण करती है। फिर अजित अपने भाषा-परिवार से बाहर निकलकर इतर भाषाओँ और भाषा-परिवारों में जा पहुँचते हैं। वहां उन देशों की सांस्कृतिक पृष्टभूमि में सम्बंधित शब्द का परीक्षणकर, पुनः समष्टिमूलक वैश्विक परिदृश्य का निर्माण कर देते हैं। यह सब रचनाकार की प्रतिभा और उसके अध्यवसाय के मणिकांचन योग से ही संभव हो सका है। व्युत्पत्तिविज्ञान की एक नयी और अनूठी समग्र शैली सामने आई है।
16.चंद्रभूषण-
[1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 .9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.]
 15.दिनेशराय द्विवेदी-[1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.]
15.दिनेशराय द्विवेदी-[1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.]
13.रंजना भाटिया-
12.अभिषेक ओझा-
[1. 2. 3.4.5 .6 .7 .8 .9 . 10]
11.प्रभाकर पाण्डेय-
10.हर्षवर्धन-
9.अरुण अरोरा-
8.बेजी-
7. अफ़लातून-
6.शिवकुमार मिश्र -
5.मीनाक्षी-
4.काकेश-
3.लावण्या शाह-
1.अनिताकुमार-
 हिंदी में शब्दों की खोज लगभग खत़्म हो गयी है. लेखक इस ज़रूरत से उठ गये हैं कि उनकी अभिव्यक्ति के पन्नों को नये शब्द कुछ रोशनी बिखेर सकते हैं. बल्कि जाने हुए शब्दों के जरिये कहानी और कविता के सीमित शिल्प को सरल समय का आईना कह कर वे नये शब्दों की ज़रूरत को खारिज़ तक कर देते हैं. लेकिन ब्लॉग्स में भूले हुए शब्दों को खोजने और कई मौजूदा शब्दों की जड़ों तक पहुंचने का काम कुछ लोग कायदे से कर रहे हैं.
अजित वाडनेकर ऐसे ही एक सिपाही हैं, जो शब्दों का सफ़र (http://shabdavali.blogspot.com/) नाम से अपना ब्लॉग चलाते हैं. उनके बारे में जानकारी अभय तिवारी के निर्मल आनंद से मिली. उन्होंने लिखा- पाया ब्लॉग जगत ने एक नया नगीना. आगे लिखा, 'वे हिंदी भाषा के संसार में एक मौलिक काम कर रहे हैं. शब्दों को उनके मूल में जाकर जांच परख रहे हैं. देशकाल और विभिन्न समाजों में उनकी यात्रा को खोल रहे हैं.` इतना काफी था हमें किसी ब्लॉग के बारे में उत्सुक करने के लिए. हम जब वहां पहुंचे, तो सचमुच ताज़ा रचनात्मकता की शीतल बूंदें वहां मोतियों की तरह बिखरी थीं.
ब्लॉग पर अपने सफ़र का आगा़ज़ वे कुछ इस तरह करते हैं, 'उत्पत्ति की तलाश में निकलें, तो शब्दों का बहुत ही दिलचस्प सफ़र सामने आता है. लाखों सालों में जैसे इंसान अपनी शक्ल बदली, सभ्यता के विकास के बाद से शब्दों ने भी अपने व्यवहार बदले. एक भाषा का शब्द दूसरी में गया और अरसे बाद एक तीसरी ही शक्ल में प्रचलित हुआ.`
आप अगर शब्दावली के पन्ने पलटेंगे, तो पाएंगे कि अजित वडनेरकर ग्राम, गंवार और संग्राम के बीच के अंतर्संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं. बगातुर और बघातुर से होते हुए बहादुर तक पहुंच रहे हैं. कुली से कुल की पहचान कर रहे हैं... और आरोही और रूहेलखंड के अर्थों में कुछ सम खोज रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकतरफा ही परोसा जा रहा है. हिंदी में शब्दों पर कम कश्मकश इधर देखने को मिले हैं, लेकिन ब्लॉग पर अजित वडनेकर से दो-दो हाथ करने वाले बहुतायत में हैं. एक का ज़िक्र यहां करते हैं.
बजरबट्टू के बारे में अजित वडनेकर ने लिखा, 'प्राचीनकाल में गुरुकुल के विद्यार्थी के लिए ही आमतौर पर वटु: या बटुक शब्द का प्रयोग किया जाता था. राजा-महाराजाओं और श्रीमंतों के यहां भी ऋषि-मुनियों के साथ ये वटु: जो उनके गुरुकुल में अध्ययन करते थे, जाते और दान पाते. बजरबट्टू भी बटुक से ही बना. बजरबट्टू आमतौर पर मूर्ख या बुद्धू को कहा जाता है. जिस शब्द में स्नेह-वात्सल्य जैसे अर्थ समये हों, उससे ही बने एक अन्य शब्द से तिरस्कार प्रकट करने वाले भाव कैसे जुड़ गये? आश्रमों में रहते हुए जो विद्यार्थी विद्याध्ययन के साथ-साथ ब्रह्मचर्यव्रत के सभी नियमों का कठोरता से पालन करता, उसे वज्रबटुक कहा जाने लगा. जाहिर है वज्र यानी कठोर और बटुक मतलब ब्रह्मचारी/विद्यार्थी. ये ब्रह्मचारी अपने गुरु के निर्देशन में वज्रसाधना करते, इसलिए वज्रबटुक कहलाये. मगर सदियां बीतने पर जब गुरुकुल और आश्रम परंपरा का ह्रास होने लगा, तब बेचारे इन बटुकों की कठोर वज्रसाधना को भी समाज ने उपहास और तिरस्कार के नजरिये से देखना शुरू किया और अच्छा-खासा वज्रबटुक हो गया बजरबट्टू यानी मूर्ख.`
लेकिन अभय तिवारी ने बजरबट्टू के इस संधान पर संदेह किया. साफ है कि शब्दों के संधान को लेकर अलग अलग आग्रह और व्याख्याएं और सूचनाएं ब्लॉग पर तुरत-फुरत एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं, और सफ़र को आगे जारी रखने में मदद मिलती है. अभय तिवारी ने प्रतिवाद किया, 'बजरबट्टू शब्द का लोकप्रिय प्रयोग बुरी नज़र से बचाने वाले एक पत्थर के अर्थ के बतौर है. रामशंकर शुक्ल 'रसाल` के भाषा शब्दकोश में भी बजरबट्टू का अर्थ है- एक पेड़ का बीज जिसे दृष्टिदोष से बचाने के लिए बच्चों को पहनाते हैं. बजर तो साफ़ साफ़ वज्र का तद्भव है, मगर बट्टू क्या है? क्या वट? क्या वटन? या वटक?`
और इस तरह एक नया भाषा विमर्श शुरू होता है, जिसमें हिंदी के कवि बोधिसत्व भी कूदते हैं. अपने ब्लॉग विनय पत्रिका में वे लिखते हैं, 'संदर्भ बजर का हो या बट्टू का, पर आप अपने बटुए को न भूलें. नहीं तो आप के हाथ से साबुन की बट्टी लेकर कोई और अपनी किस्मत चमकाएगा. फिर आप को बटुर (सिकुड़) कर रहना पड़ेगा और इसमें ठाकुर जी का बटोर (हजारी प्रसाद द्विवेदी) करने से भी कोई फायदा नहीं होगा. और आप धूल बटोरने में उम्र बिता देंगे. अच्छा हो कि यह बट्टा बन कर किसी भाव न गिरा दें जैसे कि आज कल कइयों का गिरा है.`
बजरबट्टू की इस पूरी बहस में कुल २९ बार लोग एक दूसरे से आपस में उलझे. अजित वडनेकर की पोस्ट पर चार टिप्पणियां दर्ज हैं, अभय तिवारी की पोस्ट पर बीस टिप्पणियां और बोधिसत्व की पोस्ट पर पांच टिप्पणियां दर्ज हैं. इस पूरी बहस में लंदन से अनामदास के साथ अनूप शुक्ला, इरफ़ान, अफलातून, काकेश, प्रियंकर, प्रमोद सिंह ने हिस्सा लिया. और भी कई नाम हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी.
सवाल असहमतियों के लोकतांत्रिक गंठजोड़ का जितना है, उससे कहीं अधिक जिसके पास जितनी चीज़ें हैं, वे आपस में साझा कर रहे हैं. नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर जैसे अखब़ारों और दूरदर्शन, ज़ी न्यूज़, आजतक और स्टार न्यूज़ के साथ काम करते हुए अजित वडनेरकर पिछले बाइस सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. इतिहास और संस्कृति से उनका गहरा लगाव है, लेकिन ये अखब़ार आज जो उनका पेशा है, उसमें किसी काम का नहीं. लेकिन जो है, उसे समेटना है, बांटना है और ब्लॉग इसके लिए उन्हें सबसे सटीक माध्यम लगा. --अविनाश [लेखक का ब्लाग है http://mohalla.blogspot.com/ ]
हिंदी में शब्दों की खोज लगभग खत़्म हो गयी है. लेखक इस ज़रूरत से उठ गये हैं कि उनकी अभिव्यक्ति के पन्नों को नये शब्द कुछ रोशनी बिखेर सकते हैं. बल्कि जाने हुए शब्दों के जरिये कहानी और कविता के सीमित शिल्प को सरल समय का आईना कह कर वे नये शब्दों की ज़रूरत को खारिज़ तक कर देते हैं. लेकिन ब्लॉग्स में भूले हुए शब्दों को खोजने और कई मौजूदा शब्दों की जड़ों तक पहुंचने का काम कुछ लोग कायदे से कर रहे हैं.
अजित वाडनेकर ऐसे ही एक सिपाही हैं, जो शब्दों का सफ़र (http://shabdavali.blogspot.com/) नाम से अपना ब्लॉग चलाते हैं. उनके बारे में जानकारी अभय तिवारी के निर्मल आनंद से मिली. उन्होंने लिखा- पाया ब्लॉग जगत ने एक नया नगीना. आगे लिखा, 'वे हिंदी भाषा के संसार में एक मौलिक काम कर रहे हैं. शब्दों को उनके मूल में जाकर जांच परख रहे हैं. देशकाल और विभिन्न समाजों में उनकी यात्रा को खोल रहे हैं.` इतना काफी था हमें किसी ब्लॉग के बारे में उत्सुक करने के लिए. हम जब वहां पहुंचे, तो सचमुच ताज़ा रचनात्मकता की शीतल बूंदें वहां मोतियों की तरह बिखरी थीं.
ब्लॉग पर अपने सफ़र का आगा़ज़ वे कुछ इस तरह करते हैं, 'उत्पत्ति की तलाश में निकलें, तो शब्दों का बहुत ही दिलचस्प सफ़र सामने आता है. लाखों सालों में जैसे इंसान अपनी शक्ल बदली, सभ्यता के विकास के बाद से शब्दों ने भी अपने व्यवहार बदले. एक भाषा का शब्द दूसरी में गया और अरसे बाद एक तीसरी ही शक्ल में प्रचलित हुआ.`
आप अगर शब्दावली के पन्ने पलटेंगे, तो पाएंगे कि अजित वडनेरकर ग्राम, गंवार और संग्राम के बीच के अंतर्संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं. बगातुर और बघातुर से होते हुए बहादुर तक पहुंच रहे हैं. कुली से कुल की पहचान कर रहे हैं... और आरोही और रूहेलखंड के अर्थों में कुछ सम खोज रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकतरफा ही परोसा जा रहा है. हिंदी में शब्दों पर कम कश्मकश इधर देखने को मिले हैं, लेकिन ब्लॉग पर अजित वडनेकर से दो-दो हाथ करने वाले बहुतायत में हैं. एक का ज़िक्र यहां करते हैं.
बजरबट्टू के बारे में अजित वडनेकर ने लिखा, 'प्राचीनकाल में गुरुकुल के विद्यार्थी के लिए ही आमतौर पर वटु: या बटुक शब्द का प्रयोग किया जाता था. राजा-महाराजाओं और श्रीमंतों के यहां भी ऋषि-मुनियों के साथ ये वटु: जो उनके गुरुकुल में अध्ययन करते थे, जाते और दान पाते. बजरबट्टू भी बटुक से ही बना. बजरबट्टू आमतौर पर मूर्ख या बुद्धू को कहा जाता है. जिस शब्द में स्नेह-वात्सल्य जैसे अर्थ समये हों, उससे ही बने एक अन्य शब्द से तिरस्कार प्रकट करने वाले भाव कैसे जुड़ गये? आश्रमों में रहते हुए जो विद्यार्थी विद्याध्ययन के साथ-साथ ब्रह्मचर्यव्रत के सभी नियमों का कठोरता से पालन करता, उसे वज्रबटुक कहा जाने लगा. जाहिर है वज्र यानी कठोर और बटुक मतलब ब्रह्मचारी/विद्यार्थी. ये ब्रह्मचारी अपने गुरु के निर्देशन में वज्रसाधना करते, इसलिए वज्रबटुक कहलाये. मगर सदियां बीतने पर जब गुरुकुल और आश्रम परंपरा का ह्रास होने लगा, तब बेचारे इन बटुकों की कठोर वज्रसाधना को भी समाज ने उपहास और तिरस्कार के नजरिये से देखना शुरू किया और अच्छा-खासा वज्रबटुक हो गया बजरबट्टू यानी मूर्ख.`
लेकिन अभय तिवारी ने बजरबट्टू के इस संधान पर संदेह किया. साफ है कि शब्दों के संधान को लेकर अलग अलग आग्रह और व्याख्याएं और सूचनाएं ब्लॉग पर तुरत-फुरत एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं, और सफ़र को आगे जारी रखने में मदद मिलती है. अभय तिवारी ने प्रतिवाद किया, 'बजरबट्टू शब्द का लोकप्रिय प्रयोग बुरी नज़र से बचाने वाले एक पत्थर के अर्थ के बतौर है. रामशंकर शुक्ल 'रसाल` के भाषा शब्दकोश में भी बजरबट्टू का अर्थ है- एक पेड़ का बीज जिसे दृष्टिदोष से बचाने के लिए बच्चों को पहनाते हैं. बजर तो साफ़ साफ़ वज्र का तद्भव है, मगर बट्टू क्या है? क्या वट? क्या वटन? या वटक?`
और इस तरह एक नया भाषा विमर्श शुरू होता है, जिसमें हिंदी के कवि बोधिसत्व भी कूदते हैं. अपने ब्लॉग विनय पत्रिका में वे लिखते हैं, 'संदर्भ बजर का हो या बट्टू का, पर आप अपने बटुए को न भूलें. नहीं तो आप के हाथ से साबुन की बट्टी लेकर कोई और अपनी किस्मत चमकाएगा. फिर आप को बटुर (सिकुड़) कर रहना पड़ेगा और इसमें ठाकुर जी का बटोर (हजारी प्रसाद द्विवेदी) करने से भी कोई फायदा नहीं होगा. और आप धूल बटोरने में उम्र बिता देंगे. अच्छा हो कि यह बट्टा बन कर किसी भाव न गिरा दें जैसे कि आज कल कइयों का गिरा है.`
बजरबट्टू की इस पूरी बहस में कुल २९ बार लोग एक दूसरे से आपस में उलझे. अजित वडनेकर की पोस्ट पर चार टिप्पणियां दर्ज हैं, अभय तिवारी की पोस्ट पर बीस टिप्पणियां और बोधिसत्व की पोस्ट पर पांच टिप्पणियां दर्ज हैं. इस पूरी बहस में लंदन से अनामदास के साथ अनूप शुक्ला, इरफ़ान, अफलातून, काकेश, प्रियंकर, प्रमोद सिंह ने हिस्सा लिया. और भी कई नाम हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी.
सवाल असहमतियों के लोकतांत्रिक गंठजोड़ का जितना है, उससे कहीं अधिक जिसके पास जितनी चीज़ें हैं, वे आपस में साझा कर रहे हैं. नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर जैसे अखब़ारों और दूरदर्शन, ज़ी न्यूज़, आजतक और स्टार न्यूज़ के साथ काम करते हुए अजित वडनेरकर पिछले बाइस सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. इतिहास और संस्कृति से उनका गहरा लगाव है, लेकिन ये अखब़ार आज जो उनका पेशा है, उसमें किसी काम का नहीं. लेकिन जो है, उसे समेटना है, बांटना है और ब्लॉग इसके लिए उन्हें सबसे सटीक माध्यम लगा. --अविनाश [लेखक का ब्लाग है http://mohalla.blogspot.com/ ]
 शब्दों के प्रति लापरवाही से भरे इस दौर में हर शब्द को अर्थविहीन बनाने का चलन आम हो गया है। इस्तेमाल किए जाने भर के लिए ही शब्दों का वाक्यों के बाच में आना जाना हो रहा है, खासकर पत्रारिता ने सरल शब्दों के चुनाव क क्रम में कई सारे शब्दों को हमेशा के लिए स्मृति से बाहर कर दिया। जो बोला जाता है वही तो लिखा जाएगा। तभी तो सर्वजन से संवाद होगा। लेकिन क्या जो बोला जा रहा है, वही अर्थसहित समझ लिया जा रहा है ? उर्दू का एक शब्द है खुलासा । इसका असली अर्थ और इस्तेमाल के संदर्भ की दूरी को कोई नहीं पाट सका। इसीलिए बीस साल से पत्रकारिता में लगा एक शख्स शब्दों का साथी बन गया है। वो शब्दों के साथ सफर पर निकला है। अजित वडनेरकर। ब्लॉग का पता है http://shabdavali.blogspot.com दो साल से चल रहे इस ब्लॉग पर जाते ही तमाम तरह के शब्द अपने पूरे खानदान और अड़ोसी-पड़ोसी के साथ मौजूद होते हैं। मसलन संस्कृत से आया ऊन अकेला नहीं है। वह ऊर्ण से तो बना है, लेकिन उसके खानदान में उरा (भेड़), उरन (भेड़) ऊर्णायु (भेड़), ऊर्णु (छिपाना)आदि भी हैं । इन तमाम शब्दों का अर्थ है ढांकना या छिपाना। एक भेड़ जिस तरह से अपने बालों से छिपी रहती है, उसी तरह अपने शरीर को छुपाना या ढांकना। और जिन बालों को आप दिन भर संवारते हैं वह तो संस्कृत-हिंदी का नहीं बल्कि हिब्रू से आया है। जिनके बाल नहीं होते, उन्हें समझना चाहिए कि बाल मेसोपोटामिया की सभ्यता के धूलकणों में लौट गया है। गंजे लोगों को गर्व करना चाहिए। इससे पहले कि आप इस जानकारी पर हैरान हों अजित वडनेरकर बताते हैं कि जिस नी धातु से नैन शब्द शब्द का उद्गम हुआ है, उसी से न्याय का भी हुआ है। संस्कृत में अरबी जबां और वहां से हिंदी-उर्दू में आए रकम शब्द का मतलब सिर्फ नगद नहीं बल्कि लोहा भी है। रुक्कम से बना रकम जसका मतलब होता है सोना या लोहा । कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का नाम भी इस रुक्म से बना है जिससे आप रकम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम शब्दों का यह संग्रहालय कमाल का लगता है। इस ब्लॉग के पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी अजब -गजब हैं। रवि रतलामी लिखते हैं कि किसी हिंदी चिट्ठे को हमेशा के लिए जिंदा देखना चाहेंगे तो वह है शब्दों का सफर । अजित वडनेरकर अपने बारे में बताते हुए लिखते हैं कि शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर भाषा विज्ञानियों का नज़रिया अलग अलग होता है। मैं भाषाविज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जज्बा उत्पति की तलाश में निकलें तो शब्दों का एक दिलचस्प सफर नजर आता है। अजित की विनम्रता जायज़ भी है और ज़रूरी भी है क्योंकि शब्दों को बटोरने का काम आप दंभ के साथ तो नहीं कर सकते। इसीलिए वे इनके साथ घूमते-फिरते हैं। घूमना-फिरना भी तो यही है कि जो आपका नहीं है, आप उसे देखने- जानने की कोशिश करते हैं। वरना कम लोगों को याद होगा कि मुहावरा अरबी शब्द हौर से आया है, जिसका अर्थ होता है परस्पर वार्तालाप, संवाद । शब्दों को लेकर जब बहस होती है तो यह ब्लॉग और दिलचस्प होने लगता है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा का एक लोकप्रिय लैंडमार्क है- अट्टा बाजार। इसके बारे में एक ब्लॉगर साथी अजित वडनेरकर को बताता है कि इसका नाम अट्टापीर के कारण अट्टा बाजार है, लेकिन अजित बताते हैं कि अट्ट से ही बना अड्डा । अट्ट में ऊंचाई, जमना, अटना जैसे भाव हैं, लेकिन अट्टा का मतलब तो बाजार होता है। अट्टा बाजार । तो पहले से बाजार है उसके पीछे एक और बाजार । बाजार के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द हाट भी अट्टा से ही आया है। इसलिए हो सकता है कि अट्टापीर का नामकरण भी अट्ट या अड्डे से हुआ हो। बात कहां से कहा पहुंच जाती है। बल्कि शब्दों के पीछे-पीछे अजित पहुंचने लगते हैं। वो शब्दों को भारी-भरकम बताकर उन्हें ओबेसिटी के मरीज की तरह खारिज नहीं करते। उनका वज़न कम कर दिमाग में घुसने लायक बना देते हैं। हिंदी ब्लॉगिंग की विविधता से नेटयुग में कमाल की बौद्धिक संपदा बनती जा रही है। टीवी पत्रकारिता में इन दिनों अनुप्रास और युग्म शब्दों की भरमार है। जो सुनने में ठीक लगे और दिखने में आक्रामक। रही बात अर्थ की तो इस दौर में सभी अर्थ ही तो ढूंढ़ रहे हैं। इस पत्रकारिता का अर्थ क्या है? अजित ने अपनी गाड़ी सबसे पहले स्टार्ट कर दी और अर्थ ढूंढ़ने निकल पड़े हैं। --रवीशकुमार [लेखक का ब्लाग है http://naisadak.blogspot.com/ ]
शब्दों के प्रति लापरवाही से भरे इस दौर में हर शब्द को अर्थविहीन बनाने का चलन आम हो गया है। इस्तेमाल किए जाने भर के लिए ही शब्दों का वाक्यों के बाच में आना जाना हो रहा है, खासकर पत्रारिता ने सरल शब्दों के चुनाव क क्रम में कई सारे शब्दों को हमेशा के लिए स्मृति से बाहर कर दिया। जो बोला जाता है वही तो लिखा जाएगा। तभी तो सर्वजन से संवाद होगा। लेकिन क्या जो बोला जा रहा है, वही अर्थसहित समझ लिया जा रहा है ? उर्दू का एक शब्द है खुलासा । इसका असली अर्थ और इस्तेमाल के संदर्भ की दूरी को कोई नहीं पाट सका। इसीलिए बीस साल से पत्रकारिता में लगा एक शख्स शब्दों का साथी बन गया है। वो शब्दों के साथ सफर पर निकला है। अजित वडनेरकर। ब्लॉग का पता है http://shabdavali.blogspot.com दो साल से चल रहे इस ब्लॉग पर जाते ही तमाम तरह के शब्द अपने पूरे खानदान और अड़ोसी-पड़ोसी के साथ मौजूद होते हैं। मसलन संस्कृत से आया ऊन अकेला नहीं है। वह ऊर्ण से तो बना है, लेकिन उसके खानदान में उरा (भेड़), उरन (भेड़) ऊर्णायु (भेड़), ऊर्णु (छिपाना)आदि भी हैं । इन तमाम शब्दों का अर्थ है ढांकना या छिपाना। एक भेड़ जिस तरह से अपने बालों से छिपी रहती है, उसी तरह अपने शरीर को छुपाना या ढांकना। और जिन बालों को आप दिन भर संवारते हैं वह तो संस्कृत-हिंदी का नहीं बल्कि हिब्रू से आया है। जिनके बाल नहीं होते, उन्हें समझना चाहिए कि बाल मेसोपोटामिया की सभ्यता के धूलकणों में लौट गया है। गंजे लोगों को गर्व करना चाहिए। इससे पहले कि आप इस जानकारी पर हैरान हों अजित वडनेरकर बताते हैं कि जिस नी धातु से नैन शब्द शब्द का उद्गम हुआ है, उसी से न्याय का भी हुआ है। संस्कृत में अरबी जबां और वहां से हिंदी-उर्दू में आए रकम शब्द का मतलब सिर्फ नगद नहीं बल्कि लोहा भी है। रुक्कम से बना रकम जसका मतलब होता है सोना या लोहा । कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का नाम भी इस रुक्म से बना है जिससे आप रकम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम शब्दों का यह संग्रहालय कमाल का लगता है। इस ब्लॉग के पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी अजब -गजब हैं। रवि रतलामी लिखते हैं कि किसी हिंदी चिट्ठे को हमेशा के लिए जिंदा देखना चाहेंगे तो वह है शब्दों का सफर । अजित वडनेरकर अपने बारे में बताते हुए लिखते हैं कि शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर भाषा विज्ञानियों का नज़रिया अलग अलग होता है। मैं भाषाविज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जज्बा उत्पति की तलाश में निकलें तो शब्दों का एक दिलचस्प सफर नजर आता है। अजित की विनम्रता जायज़ भी है और ज़रूरी भी है क्योंकि शब्दों को बटोरने का काम आप दंभ के साथ तो नहीं कर सकते। इसीलिए वे इनके साथ घूमते-फिरते हैं। घूमना-फिरना भी तो यही है कि जो आपका नहीं है, आप उसे देखने- जानने की कोशिश करते हैं। वरना कम लोगों को याद होगा कि मुहावरा अरबी शब्द हौर से आया है, जिसका अर्थ होता है परस्पर वार्तालाप, संवाद । शब्दों को लेकर जब बहस होती है तो यह ब्लॉग और दिलचस्प होने लगता है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा का एक लोकप्रिय लैंडमार्क है- अट्टा बाजार। इसके बारे में एक ब्लॉगर साथी अजित वडनेरकर को बताता है कि इसका नाम अट्टापीर के कारण अट्टा बाजार है, लेकिन अजित बताते हैं कि अट्ट से ही बना अड्डा । अट्ट में ऊंचाई, जमना, अटना जैसे भाव हैं, लेकिन अट्टा का मतलब तो बाजार होता है। अट्टा बाजार । तो पहले से बाजार है उसके पीछे एक और बाजार । बाजार के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द हाट भी अट्टा से ही आया है। इसलिए हो सकता है कि अट्टापीर का नामकरण भी अट्ट या अड्डे से हुआ हो। बात कहां से कहा पहुंच जाती है। बल्कि शब्दों के पीछे-पीछे अजित पहुंचने लगते हैं। वो शब्दों को भारी-भरकम बताकर उन्हें ओबेसिटी के मरीज की तरह खारिज नहीं करते। उनका वज़न कम कर दिमाग में घुसने लायक बना देते हैं। हिंदी ब्लॉगिंग की विविधता से नेटयुग में कमाल की बौद्धिक संपदा बनती जा रही है। टीवी पत्रकारिता में इन दिनों अनुप्रास और युग्म शब्दों की भरमार है। जो सुनने में ठीक लगे और दिखने में आक्रामक। रही बात अर्थ की तो इस दौर में सभी अर्थ ही तो ढूंढ़ रहे हैं। इस पत्रकारिता का अर्थ क्या है? अजित ने अपनी गाड़ी सबसे पहले स्टार्ट कर दी और अर्थ ढूंढ़ने निकल पड़े हैं। --रवीशकुमार [लेखक का ब्लाग है http://naisadak.blogspot.com/ ]
मुहावरा अरबी के हौर शब्द से जन्मा है जिसके मायने हैं परस्पर वार्तालाप, संवाद।
लंबी ज़ुबान -इस बार जानते हैं ज़ुबान को जो देखते हैं कितनी लंबी है और कहां-कहा समायी है। ज़बान यूं तो मुँह में ही समायी रहती है मगर जब चलने लगती है तो मुहावरा बन जाती है । ज़बान चलाना के मायने हुए उद्दंडता के साथ बोलना। ज्यादा चलने से ज़बान पर लगाम हट जाती है और बदतमीज़ी समझी जाती है। इसी तरह जब ज़बान लंबी हो जाती है तो भी मुश्किल । ज़बान लंबी होना मुहावरे की मूल फारसी कहन है ज़बान दराज़ करदन यानी लंबी जीभ होना अर्थात उद्दंडतापूर्वक बोलना।
दांत खट्टे करना- किसी को मात देने, पराजित करने के अर्थ में अक्सर इस मुहावरे का प्रयोग होता है। दांत किरकिरे होना में भी यही भाव शामिल है। दांत टूटना या दांत तोड़ना भी निरस्त्र हो जाने के अर्थ में प्रयोग होता है। दांत खट्टे होना या दांत खट्टे होना मुहावरे की मूल फारसी कहन है -दंदां तुर्श करदन
अक्ल गुम होना- हिन्दी में बुद्धि भ्रष्ट होना, या दिमाग काम न करना आदि अर्थों में अक्ल गुम होना मुहावरा खूब चलता है। अक्ल का घास चरने जाना भी दिमाग सही ठिकाने न होने की वजह से होता है। इसे ही अक्ल का ठिकाने न होना भी कहा जाता है। और जब कोई चीज़ ठिकाने न हो तो ठिकाने लगा दी जाती है। जाहिर है ठिकाने लगाने की प्रक्रिया यादगार रहती है। बहरहाल अक्ल गुम होना फारसी मूल का मुहावरा है और अक्ल गुमशुदन के तौर पर इस्तेमाल होता है।
दांतों तले उंगली दबाना - इस मुहावरे का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। डॉ भोलानाथ तिवारी के मुताबिक इस मुहावरे की आमद हिन्दी में फारसी से हुई है फारसी में इसका रूप है- अंगुश्त ब दन्दां ।