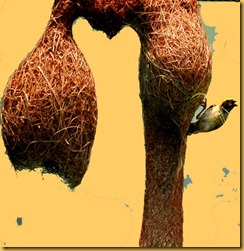[ शब्द संदर्भ- असबाब, अहदी, मुसद्दी, मुनीम, जागीरदार, तहसीलदार, वज़ीर, सर्राफ़, नौकर, चाकर, नायब, फ़ौजदार, पंसारी, व्यापारी, दुकानदार, बनिया-बक्काल, क़ानूनगो, लवाजमा, चालान, जमादार, भंडारी, कोठारी, किरानी, चीज़, गोदाम, अमीर, वायसराय ]
पिछली कड़ी- मोदी की जन्मकुंडली
मोदी की अर्थवत्ता में शामिल भावों पर गौर करें तो इसका रिश्ता आपूर्ति, भंडार, स्टोर, राशन, दुकान, रसद, मिलिट्री सप्लाई, किराना, राजस्व, कर वसूली आदि से जुड़ता है । इन आशयों से जुड़े शब्दों की एक लम्बी शृंखला सेमिटिक धातु मीम-दाल-दाल (م د د ) यानी m-d-d से बनी है जिसमें आपूर्ति, सप्लाई, सहायता, सहारा, फैलाव जैसे भाव है । गौर करें हिन्दी में सहायता का लोकप्रिय पर्याय ‘मदद’ है जो इसी कड़ी से जुड़ा है । मद्द’ में निहित आपूर्ति या सहायता के भाव का विस्तार मदद में हैं जिससे मददगार, मददख़्वाह जैसे शब्द बने हैं । इसी कड़ी में आता है ‘इमदाद’ जिसका अर्थ भी आपूर्ति, सहायता, आश्रय, हिमायत अथवा सहारा होता है ।
मद्द धातु से बने शब्दों में एक और दिलचस्प सब्द की शिनाख़्त होती है । बहीखातों की पहचान लम्बे-लम्बे कॉलम होते हैं जिनमें हिसाब-किताब लिखा जाता है । अरबी में इसके लिए ‘मद्द’ शब्द है । घिसते घिसते हिन्दी में यह ‘मद’ हो गया । हिन्दी में इसका प्रयोग जिन अर्थों में होता है उसका आशय खाता, पेटा, हेड या शीर्षक है जैसे- “यह रकम किस ‘मद’ में डाली जाए” या “मरम्मत वाली ‘मद’ मे कुछ राशि बची है” आदि । मद / मद्द के कॉलम, स्तम्भ या सहारा वाले अर्थ में अन्द्रास रज्की के अरबी व्युत्पत्ति कोश में अलहदा धातु ऐन-मीम-दाल से बताई गई है । इससे बने इमादा, इमाद, अमीद, अमूद और उम्दा जैसे शब्द हैं जिनमें सहारा, मुखिया, स्तम्भ, प्रमुख, विश्वसनीय, प्रतिनिधि जैसे भाव भी हैं, अलबत्ता ये हिन्दी में प्रचलित नहीं हैं । सम्भव है यह मद्द की समरूप धातु हो ।
मोदी शब्द की व्युत्पत्ति को मद्द से मानने की बड़ी वजह है इसमें निहित वे भाव जिनसे मोदी की अर्थवत्ता स्थापित होती है । ‘मद’ तो हुआ खाता मगर इसका ‘मद्द’ रूप भी हिन्दी में नज़र आता है जैसे मद्देनज़र, मद्देअमानत आदि । मद्देनज़र का अर्थ है निग़ाह में रखना । ‘मदद’ में जहाँ सहायता का भाव है वहीं आपूर्ति भी उसमें निहित है । ‘मदद’ अपने आप में सहारा भी है सो ‘मदद’ में निहित ‘मद्द’ पहले कॉलम या स्तम्भ हुआ फिर यह बहीखातों का कॉलम या खाना हुआ और फिर इसे मदद की अर्थवत्ता मिली । अरबी में एक शब्द है ‘मद्दा’ जिसका अर्थ है विस्तार, फैलाव, सहारा वहीं इसमें सामान, वस्तु, चीज़, पदार्थ अथवा मवाद आदि की अर्थवत्ता भी है । शरीर के भीतर जख्म होने पर जब वह पकता है तो उसका आकार फूलता है । प्रसंगवश ‘मवाद’ शब्द भी अरबी का है और इसी मूल से निकला है । ‘मद्द’ में निहित फैलाव, विस्तार इसमें निहित है । ध्यान रहे आपूर्ति में भी विस्तार, फैलाव की अर्थवत्ता है । किसी स्थान पर किसी चीज़ की आपूर्ति से फैलाव होता है । गुब्बारे में हवा की आपूर्ति से समझें । भोजन करने पर पेट के फूलने से समझें । इसी तरह विशाल क्षेत्र में राशन की आपूर्ति में भी फैलाव का वही आशय है ।
यूँ मुग़लदौर में एक सरकारी विभाग ‘मोदीखाना’ भी प्रसिद्ध था जिसका अर्थ था रसद-आपूर्ति विभाग । हिन्दुस्तानी – फ़ारसी कोशों में मोदीखाना शब्द मिलता है जिसका अर्थ भण्डारगृह , किराना-स्टोर, अनाज की आढ़त, granary या commissariat ( कमिसरियत, सेना रसद विभाग ) मिलता है । हालाँकि इन्स्टीट्यूट ऑफ सिख स्टडीज़ के डॉ. कृपाल सिंह ने अपनी पुस्तक सिख्स एंड अफ़गान्स में ‘मोदी’ को अरबी शब्द माना है और इसका अर्थ “भुगतान किया जा चुका” बताया है । इसी पुस्तक में वे ‘मोदीखाना’ के बारे में बताते हैं कि यह दरअसल मुस्लिम दौर की उन सरकारों में एक महत्वपूर्ण विभाग था जहाँ किन्हीं कारणों से मौद्रिक लेन-देन कम होता था और भू-राजस्व का भुगतान जिन्सी तौर पर किया जाता था । अर्थात मुद्रा के बदले अनाज, राशन, पशु आदि दे दिए जाते थे । सरकार इसे ही महसूल समझ कर रख लेती थी । इसी मोदीखाने का प्रमुख ‘मोदी’ कहलाता था । यह ‘मोदी’ कर वसूल करता था । उसे जमा करता था और फिर जमा की गई जिंसों को वह शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेच भी सकता था । ज़ाहिर है इस नाम के पीछे मद्दा में निहित वस्तु, सामग्री, जिंस, चीज़ जैसे आशय ही व्युत्पत्तिक आधार हैं । प्रसंगवश सुलतानपुर के नवाब दौलत खां लोधी के मोदीखाने में अपने शुरुआती जीवन में गुरुनानक भंडारी (मोदी) के पद पर थे जहाँ खाद्यान्न के रूप में लगान जमा किया जाता था ।
सेनाओं में प्राचीनकाल से ही यह परिपाटी रही है कि कूच करते वक्त उनके साथ दुनियाजहान का असबाब भी चलता था । चालू भाषा में जिसे लवाजमा या फौजफाटा कहते हैं उसका तात्पर्य यही है । मुग़ल दौर में जब फौज चलती थी उसके साथ पंसारी की दुकान भी होती थी जिसे मोदीख़ाना कहते थे । दवाईखाना, मरम्मतखाना, फराशखाना जैसे विभागों में ही एक विभाग मोदीखाना था । स्थायी तौर पर किसी श्रेष्ठी को सेना में रसद आपूर्ति का काम मिल जाता था और कभी शासन की तरफ़ से ही प्रत्येक बड़े शहर में वणिकों को फौज को राशन पहुँचाने का अनुबंध मिल जाता था । सरकार के स्वामीभक्त व्यवसायी, प्रभावशाली धनिक ऐसे करार (ठेके) पाने के लिए जोड़-तोड़ करते थे । मगर उसकी मुश्किलें भी थीं । ये काम पाने के लिए उन्हें आज की ही तरह से सरकार के असरदार लोगों की जेबें गर्म करनी पड़ती थीं । आठवीं-नवीं सदी के भारत में भ्रष्टाचार के कई नमूने शूद्रक के ‘मृच्छकटिकम’ नाटक से भी पता चलते हैं ।
आचार्य विष्णुशर्मा लिखित पंचतन्त्र में इसका उल्लेख है जिससे पता चलता है कि सेना में रसद आपूर्ति का काम प्राचीनकाल से ही मोटी कमाई वाला माना जाता था । पंचतन्त्र की संस्कृत – हिन्दी व्याख्या में श्यामाचरण पाण्डेय लिखते हैं- गौष्ठिककर्मनियुक्तः श्रेष्ठी चिन्तयति चेतसा हृष्टः। वसुधा वसुसम्पूर्णा मयाSद्य लब्धा किमन्येन ।। अर्थात “मोदी का काम करने वाला व्यापारी जब किसी राजकीय सेना आदि को रसद पहुँचाने का कार्य पा जाता है तो प्रसन्न होकर अपने मन में सोचता है कि आज मैने पृथ्वी पर सम्पूर्ण धन ही प्राप्त कर लिया है । पुनः निश्चित होकर लोगों को लूटता है ।” आज के दौर के बड़े कारोबारियों के पुरखों ने प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में रसद आपूर्ति ठेकों में करोड़ों के वारे-न्यारे किए थे, यह किसी से छुपा नहीं है । सेना सहित विभिन्न विभागों के कैंटीन और रेलवे की खानपान सेवा जैसी व्यवस्थाएँ दरअसल “मोदीखाना” जैसी प्राचीन आपूर्ति सेवाओं के ही बदले हुए रूप हैं । यूँ ‘मोद’ से भी ‘मोदी’ का रिश्ता जोड़ा जा सकता है क्योंकि उसके सारे प्रयत्न खुद के आमोद-प्रमोद के लिए होते हैं ।-समाप्त
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
अभी और बाकी है। दिलचस्प विवरण पढ़ें आगे...