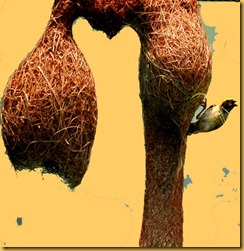त्येक बोली-भाषा में कुछ अनोखे शब्द होते हैं। मालवी भाषा में देखने के लिए एक खास क्रिया का प्रयोग होता है- ‘टिपना’ जैसे- “थाँके कम टिपे काँई?” अर्थात तुझे कम दिखता है क्या? यह ‘टिप’ कहाँ से आ रहा है? गौर करें प्रचीनकाल से ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य रहा है। अन्तरिक्ष की ओर ताकना प्रागैतिहासिक काल से मनुष्य का प्रिय शगल रहा। ऊष्मा, ऊर्जा, चमक ये सब अग्नि के गुणधर्म हैं। सूर्य उगने पर ही मनुष्य के सामने दृष्यजगत उजागर होता था। हमें कुछ भी दिखता इसलिए हैं क्योंकि वह प्रकाशित है। यानि प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ भासित है क्योंकि वह दीप्त है। व्ह जो दीप्त है उसे हिन्दी में दिपना कहते हैं| यही मालवी का टिपना है| दिपना-टिपना के ज़रिये जानते हैं हिन्दी के कुछ बेहद प्रचलित शब्दों के बारे में।
हर भाषा में किन्हीं ध्वनियों में बदलाव का अलग अंदाज़ होता है जिससे शब्दों का विकास होता है। हिन्दी-ईरानी में एक ही वर्णक्रम की ध्वनियों में बदलाव होता जाता है जैसे ‘प’ और ‘व’ में परस्पर बदलाव होता है। उदाहरण के लिए वैदिक शब्द ‘तप्’ को लें जिसमें अग्नि, चमक, ऊर्जा के साथ कष्ट, साधना, अभ्यास का भाव भी है। इससे ही तपस्वी, तपस्या, तापस जैसे शब्द बने। ‘तप’ का विकास ताप है। हिन्दी-फ़ारसी में ‘ताप’ से ‘ताव’ बनता है जिसमें गर्मी का भाव है। ‘ताव’ से ही मालवी-राजस्थानी में ‘तावड़ा’ बनता है यानी धूप। ‘तपः’ का एक रूप फारसी में तबाह बनता है जिसका अर्थ है बर्बादी, विनष्ट, जर्जर, ध्वस्त, निर्जन, वीरान आदि। समझा जा सकता है कि किसी जमाने में अग्नि से जुड़ी विभीषिका को ही तबाही कहा जाता रहा होगा।
हम जिसे दिन कहते हैं उसका एक रूप दिवस है। दिवस का मूल दिव है। गौर करें, यह दिव दरअसल दिप् रहा होगा और यह भी कि तप, ताप जैसे शब्द इसी दिप् से विकसित हैं। वैदिकी में दिप् नहीं है, दीप् क्रिया है किन्तु इसका पूर्वरूप दिप् ज़रूर रहा होगा क्योंकि कालान्तर में ऐसे अनेक वैदिक-संस्कृत शब्दरूप बने जिनका मूल दिप् ही सिद्ध होता है। यही दिप्, टिपना क्रिया का मूल है। ख्यात भाषाविद् डॉ रामविलास शर्मा “भारतीय संस्कृति और हिन्दी प्रदेश-1” में ऋग्वेद के तपस् /तवस रूपों की चर्चा करते हैं। तपस् जो ऊष्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ तथा तवस् जिसका प्रयोग ऊर्जा, शक्ति के अर्थ में हुआ है, इससे साबित होता है कि दिव् का पूर्वरूप भी दिप् रहा होगा जिससे दीप् क्रिया बनी होगी जिसमें जलना, ऊर्जा, ऊष्मा, चमक, प्रकाश जैसे भाव है और इससे ही दीप, दीपक, दीवाली जैसे अनेक शब्द बने। यह साबित होता है हिन्दी की ‘दिपना’ क्रिया से जिसका अर्थ चमक, प्रकाश या प्रदीपन है। मूल भाव है दिखना। यह न माना जाए कि ‘दिपना’ का अगला रूप ‘टिपना’ है। टिपना ‘टिप’ से आ रहा है और दिपना ‘दिप’ से। ‘दिप्’ के ‘टिप्’ रूप से मालवी की ‘टिपना’ क्रिया बनी।
‘दिप’ में निहित दीप्ति, चमक, प्रकाश जैसे भाव ही ‘टिप’ में भी समाहित है। कोई चीज़ जब चमकती है तो ही नज़र आती है। हाँ, संस्कृत में इसका अर्थविस्तार भी हुआ और इसमें चमक, झलक, दिखाना, व्याख्या जैसे भाव हैं। किसी वस्तु का दीप्तिमान होना या उसका दीपन, प्रदीपन होना ही उजागर होना है। टिप से ही मालवी बोली में ‘टिपना’ शब्द बना जिसका अर्थ है दिखना। हिन्दी में ‘टिप्पणी’ या टीका-टिप्पणी शब्द भी खूब प्रचलित है। टिप्पणी का अर्थ है किसी वाक्य, वस्तु, स्थान अथवा विचार को स्पष्ट करने वाला विवरण। इस में भी मूलतः उजागर करने का ही भाव है और इसीलिए इसे टिप्पणी कहा जाता है।
‘टिपना’ पर ये टिप्पणी कैसी लगी ?
ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें
|