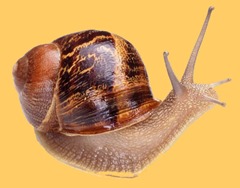| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Monday, April 3, 2023
‘नाबाद’ के बहाने ‘बाद’ की बातें
प्रस्तुतकर्ता
अजित वडनेरकर
15
कमेंट्स
पर
12:41 PM
![]() लेबल:
तकनीक,
व्यवहार
लेबल:
तकनीक,
व्यवहार
Saturday, February 4, 2017
चुभने-चुभाने की बातें
ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें
|
Wednesday, September 21, 2016
जलकुक्कड़ और तन्दूरी-चिकन
छली पोस्ट में हमने वामियों के सन्दर्भ में ‘जलकुक्कड़’ का प्रयोग किया जिस पर सफ़र के साथी प्रदीप पाराशर ने जिज्ञासा दिखाई। ‘जलकुक्कड़’ एक मुहावरा है जो आमतौर पर ईर्ष्यालु के सन्दर्भ में इस्तेमाल होता है। यूँ इसमें शक, शंका, कपट, संदेह या डाह करने का भाव है। ‘सौतिया-डाह’ वाली जलन को मुहावरे में भी खूब महसूस किया जाता है। गौर करें, ये सभी भाव अग्नि से जुड़ते हैं। संदेह, शक या शंका दरअसल एक चिंगारी है। ‘डाह’ तो सीधे-सीधे दाह का ही रूपान्तर है। संस्कृत में ‘दह’ का आशय तपन, ताप, अगन, जलन, झुलसन से है।
जलकुक्कड़ में जो जल है वह ज़ाहिर है दाह या जलन वाले ‘जल’ के अर्थ में है न कि पानी वाले अर्थ में। कुक्कड़ यानी मुर्ग़। कुक्कड़ संस्कृत के कुक्कुट का देशी रूप है। कुक्कुट का कुर्कुट रूपान्तर होकर कुक्कड़ बना, ऐसा कृपा कुलकर्णी मराठी व्युत्पत्तिकोश में लिखते हैं। वैसे कुक्कुट से कुक्कड़ बनने के लिए कुर्कुट अवतार की ज़रूरत नहीं। ‘ट’ का रूपान्तर ‘ड़’ में होने से कुक्कुट सीधे ही कुक्कड़ बन जाता है।
जलकुक्कड़ को समझने के लिए “जल-भुन जाना” मुहावरे पर गौर करें। शरीर का कोई अंग आग के सम्पर्क में आने पर झुलस जाता है। जल-भुन वाले मुहावरे में यही जलन है। दूसरा मुहावरा देखिए- “जल-भुन कर कबाब होना”। कबाब एक ऐसा व्यंजन है जिसे सीधे तन्दूर पर या तवे पर खूब अच्छी तरह भूना जाता है। जब ज्यादा ही “अच्छी तरह” भून लिया जाए तो वह जल-भुन कर कोयला हो जाता है, कबाब नहीं रह जाता।
एक अन्य पद देखिए- “तन्दूरी-मुर्ग़”। मुर्ग़े को जब आग पर सालिम भूना जाता है उसे ही तन्दूरी-मुर्ग़ कहते हैं। कहते हैं, ये बेहद लज़ीज़ होता है। अब अगर इसका हाल भी कबाब जैसा हो जाए तो? आशय ईर्ष्याग्नि से ही है। ऐसा आवेग, उत्ताप जो मौन या मुखरता से झलके। इस कुढ़न को ही ये तमाम मुहावरे अभिव्यक्त कर रहे हैं। जलकुक्कड़ में भी यही आशय है।
कई बार पूछा जाता है कि फलाने का क्या हाल है? जवाब आता है कि खबर सुनने के बाद से “तन्दूरी-मुर्ग़” हो रहे हैं। कई लोग जो स्वभाव से दूसरों की खुशहाली देख कर कुढ़ते रहते हैं, हमेशा डाह रखते हैं या अपनी ईर्ष्या का प्रदर्शन करते रहते हैं उन्हें स्थायी तौर पर जलकुक्कड़ का ख़िताब मिल जाता है। वे हमेशा ईर्ष्या के तन्दूर पर जलते रहते हैं। ईर्ष्या की आग जिसमें तप कर कुन्दन नहीं कोयला ही बनता है। ऐसे ही लोगों के लिए हिन्दी में जलोकड़ा या जलोकड़ी जैसे विशेषण भी हैं। कभी कभी सिर्फ़ जलौक भी कह दिया जाता है।
प्रसंगवश बताते चलें कि कुक्कुट दरअसल ध्वनिअनुकरण के आधार पर बना शब्द है। संस्कृत में एकवर्णी धातुक्रिया ‘कु’ में दरअसल ध्वनि अनुकरण का आशय है अर्थात कुकु कुक या कुट कुट ध्वनि करना। कोयल, कौआ, कुक्कुट और कुत्ता में ‘कु’ की रिश्तेदारी है । दरअसल विकासक्रम में मनुष्य का जिन नैसर्गिक ध्वनियों से परिचय हुआ वे ‘कु’ से संबंद्ध थीं। पहाड़ों से गिरते पानी की , पत्थरों से टकराकर बहते पानी की ध्वनि में कलकल निनाद उसने सुना। स्वाभाविक था कि इन स्वरों में उसे क ध्वनि सुनाई पड़ी इसीलिए देवनागरी के ‘क’ वर्ण में ही ध्वनि शब्द निहित है। सो मुर्ग़ का कुक्कुट नामकरण दाना चुगने की ‘कुट-कुट’ ध्वनि के चलते हुआ। अंग्रेजी का कॉक cock भी इसी आधार पर बना है।
इसे भी देखें- कुक्कुट
ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें
|
Monday, February 29, 2016
चूँ-चपड़ नई करने का...
यह जानना बेहद जरूरी है कि सवालिया निशान के दायरे में जितने भी सवाल हैं, पूरी दुनिया में ‘क’ से ही अभिव्यक्त होते हैं। इसे अंग्रेजी में 5W & 1H अथवा “पंचवकार, एक हकार” कहा जाता है। हिन्दी में ‘ककारषष्ठी’ कहा जा सकता है। यह दिलचस्प है कि संस्कृत के किम् में एक साथ तमाम प्रश्नवाची जिज्ञासाएँ समाई हुई है अर्थात क्या, क्यों, कब, कहाँ आदि...। इस किम से ही हिन्दी के तमाम प्रश्नवाची सर्वनामों यानी ‘कौन’, ‘कब’, ‘कहाँ’, ‘क्या’, ‘कैसे’, ‘किस’ आदि पैदा हुए हैं। इनमें सबका अपना-अपना महत्व है। कोई भी मानवीय जिज्ञासा इन सवालों के बिना पूरी नहीं होती। कोई भी कथा तब तक पूरी नहीं होती जब तक इस ‘ककारषष्ठी’ का समावेश उसमें न कर दिया जाए।
पत्रकारिता में तो इन शब्दों का महत्व गीता-कुरान-बाइबल से भी ज्यादा है। किसी भी घटना/ वारदात/ प्रसंग को जब तक इन कब-क्यों से न गुज़ारा जाए, उसे खबर की शक्ल में ढाला नहीं जा सकता। अफ़सोस कि आज के पत्रकार खबर लिखने से पहले ‘ककारषष्ठी’ मन्त्र का आह्वान नहीं करते। शायद शर्म आती होगी तो ‘6K’ की तरह याद कर लें, इसे भूल कर कोई खबर बन नहीं सकती और आप साख कमा नहीं सकते।
तो ‘किम्’ से जन्में ‘क्यों ‘का ही एक रूप है ‘चूँ’ जिसमें सवाल छिपे हैं। ध्यान रहे कि बच्चे ‘क’ और ‘च’ ध्वनियाँ सहज रूप से उच्चार लेते हैं मगर संयुक्त ध्वनियों का उच्चार नहीं कर पाते। यह समस्या अनेक मानव समूहों में भी होती है। नासिक्य स्पर्श के साथ क+य से बने क्यों का रूपान्तर ‘चों’ जाता है। अनेक लोग इसी प्रश्नवाचक चों को उच्चारते हैं। ‘क्यों’ का एक रूप फ़ारसी-उर्दू में ‘क्यूँ’ हो जाता है। स्वाभाविक है कि ‘क्यों’ से ‘चों’ की तरह ‘क्यूँ’ से ‘चूँ’ भी बन जाता है।
अब ‘क्यूँ’ हो या ‘चूँ’, है तो सवाल ही। ...और हमारा समाज जवाबदेही से हमेशा बचता नज़र आता है। भाषाओं के विकास में ही मानव-विकास नज़र आता है। लोकतन्त्र विरोधी समाज ही सवालों से कतराता है। “ज्यादा चूँ-चपड़ की तो...” एकाधिकारवादी, सामन्तवादी और सवालों से कतराते समाज की अभिव्यक्ति है। इसमें यह निहित है कि ज्यादा सवाल पूछेंगे, तो ख़ैर नहीं।
इस तब्सरे के बाद यह समझना मुश्किल नहीं बात बात में बोला जाने वाला अव्यय ‘चूँकि’ यूँ तो फ़ारसी का है पर ‘क्यूँकि’ का ही रूपान्तर है। हालाँकि जॉन प्लॉट्स ‘चूँ’ को फ़ारसी के ‘चिगुन’ से व्युत्पन्न मानते हैं जिसमें क्यों, कहाँ, कैसे का भाव है। सवाल यह है कि जब फ़ारसी में स्वतन्त्र रूप में ‘चि’ अव्यय मौजूद है और उसमें भी वही प्रश्नवाची आशय मौजूद है तब ‘चिगुन’ स्वयं ‘चि’ से व्युत्पन्न है जिसका रिश्ता ‘किम’ से है। शब्दों का सफ़र में पहले बताया जा चुका है कि पुरानी फ़ारसी-तुर्की में ‘किम्’ का एक रूप ‘चिम्’ होता हुआ ‘चि’ में तब्दील हुआ है।
तो चूँकि में क्योंकि वाले आशय समाहित है अर्थात ‘इसलिए’, ‘जैसे कि’, ‘कारण कि’ वगैरह आशय इससे स्पष्ट होते हैं। फ़ारसी में चूँ-चपड़ की जगह ‘चूँ-चिरा’ या ‘चूँ ओ चिरा’ पद प्रचलित है जिसका आशय है “कब, क्यों कहाँ”. इससे जो मुहावरा बनता है “चूँ-चिरा न करना” यानी बात वही ज्यादा सवाल न पूछो। हिन्दी ने इससे ही चूँ-चपड़ बना लिया। पुरानी हिन्दी में यह बतौर “चूँचरा” मौजूद है जिसका अर्थ है प्रतिरोध, विरोध, प्रतिवाद आदि।
निष्कर्ष- पत्रकारों को हमेशा चूँ-चपड़ करते रहना चाहिए यानी 'ककारषष्ठी' मन्त्र का जाप जारी रहे।
ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें
|
Friday, January 15, 2016
सुब्हान तेरी कुदरत यानी ‘सुभानअल्ला’
किन ने पी, किन ने न पी, किन किन के आगे जाम था
मुमकिन है इस मशहूर शेर को पढ़ कर आप सुभानअल्ला कह उठें। ये है ही इस लायक। पर आप ‘सुभानअल्ला’ ये सुनकर भी कहेंगे कि ‘तस्बीह’ और ‘सुभान’ दोनो बहन-भाई हैं। ‘सुभानअल्ला’ को बतौर प्रशस्तिसूचक अव्यय हिन्दी में भी बरता जाता है। यूँ इसका प्रयोग विस्मयकारी आह्लाद प्रकट करने के लिए भी होता है। यह लगभग ‘क्याब्बात’, ‘अद्भुत’ या ‘ग़ज़ब’ जैसा मामला है। यूँ सुभानअल्ला में बहुत अच्छा, धन्य-धन्य अथवा वाह-वाह जैसी बात है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सुभानअल्ला में vow factor भी है। जानते हैं सुभानअल्ला की जन्मकुण्डली।
सुभानअल्ला अरबी से बरास्ता फ़ारसी हिन्दी में आया है। यह एक शब्द नहीं बल्कि संयुक्त पद है। मूल रूप से अरबी का ‘सुब्हान’ ही हिन्दी में सुभान बन कर ढल गया। अरबी सुब्हान बना है त्रिवर्णी मूलक्रिया सबाहा ح ب س
यानी सीन-बा-हा से जिसमें परमेश्वर के गुणगान और प्रशस्ति का भाव है। इसका ही विकसित रूप है सुब्हान سبحان (सीन बा हा अलिफ़ नून) जिसका फ़ारसी रूप सोब्हान होता है और हिन्दी सुभान।
दरअसल सबाहा यानी सीन-बा-हा में जो मूल भाव है उसमें अनंत का भाव है मसलन विशाल जलराशि में तैरना, वह सब जो दृष्टिपटल के सामने है, जो नज़रों में है उसके वैभव को अनुभव करना। तैरते हुए देखने के इस भाव को हिन्दू संस्कृति में संसार को भवसागर मानने के रूपक से समझा जा सकता है। उस अनंत को निहारना, उसकी विशालता को अनुभव करते हुए उसमें बने रहने का भाव ही सबाहा का मूल है। और हासिल ? हासिल वह है जो बलदेवप्रसाद मिश्र की इस कविता के ज़रिये ज़ाहिर होता है-
जिस ओर निगाहें जाती हैं
उसके ही दर्शन पाती हैं
सम्पूर्ण दिशाएं सुख -सानी
उसका ही गौरव गाती हैं
तो सबाह से बने सुब्हान में सचमुच सुब्हान तेरी कुदरत का ही आशय है। प्रकृति से कोई पार नहीं पा सका है। प्रकृति ही ईश्वर है। जो कुछ हमने नहीं रचा, पर जो सब हमारे लिये है। ऐसी अनुभूति के बाद अगर सुभानअल्ला जैसी उक्ति ही निकलती है।
इसी सबाहा से विकसित हुआ एक और शब्द है तस्बीह यानी सुमिरनी जिसका जन्म सुमिरन से हुआ। विश्व की कई प्राचीन संस्कृतियों में नाम स्मरण की परम्परा रही है। इस्लाम में भी नाम स्मरण का रिवाज़ है। परम्परा के अनुसार सुमिरनी को हाथ में पकड़ कर उस पर एक छोटी सफेद थैली डाल ली जाती है। तर्जनी उंगली और अंगूठे की मदद से नाम स्मरण करते हुए सुमिरनी के दानों को लगातार आगे बढ़ाया जाता है। सुमिरनी दरअसल एक उपकरण है जो नामस्मरण की आवृत्तियों का स्मरण भक्त को कराती है।
संस्कृत के स्मरण से विकसित है सुमिरन। स्मरण > सुमिरण > सुमिरन के क्रम में इसका विकास हुआ। पंजाबी में इसका रूप है ‘सिमरन’ जहाँ प्रॉपर नाऊन की तरह भी इसका प्रयोग होता है। व्यक्तिनाम की तरह स्त्री या पुरुष के नाम की तरह सिमरन का प्रयोग होता है। बहुतांश हिन्दीवाले पंजाबी के ‘सिमरन’ की संस्कृत के ‘स्मरण’ से रिश्तेदारी से अनजान हैं क्योंकि सुमिरन की तरह से पंजाबी के सिमरन का प्रयोग हिन्दीवाले नहीं करते हैं बल्कि उसे सिर्फ व्यक्तिनाम के तौर पर ही जानते हैं। स्मरण शब्द बना है संस्कृत की ‘स्मर्’ धातु से। मोनियर विलियम्स के संस्कृत इंग्लिश कोश के मुताबिक स्मर् में याद करना, न भूलना, कंठस्थ करना, याददाश्त जैसे भाव हैं। अंग्रेजी के मेमोरी से इसकी रिश्तेदारी है। डॉ रामविलास शर्मा के मुताबिक लैटिन के मैमॉर् अर्थात स्मृति में ‘मर्’ के स्थान पर मॉर है। संस्कृत के स्मर, स्मरण, स्मृति में स-युक्त यही मर् है।
तो जब कभी किसी अनिवर्चनीय अनुभव से गुज़रें, किसी अनोखेपन के लिए मुँह से प्रशस्तिसूचक ‘वाह’ निकले तो सुभानअल्ला कहने में गुरेज़ न करें। और हाँ, खुदा की कुदरत को भी सुब्हान कहें और “मेरे महबूब को किसने बनाया” ये पहेली खुदा को बूझने दीजिए।
ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें
|
प्रस्तुतकर्ता
अजित वडनेरकर
1 कमेंट्स
पर
11:48 PM
![]() लेबल:
god and saints,
इस्लाम islam,
उपकरण,
धर्म,
वस्तु,
व्यवहार
लेबल:
god and saints,
इस्लाम islam,
उपकरण,
धर्म,
वस्तु,
व्यवहार
Monday, December 28, 2015
बात तफ़सील की...
तफ़सील को थोड़ा तफ़सील से समझा जाए। तफ़सील का रिश्ता यूँ तो अरबी शब्द फ़साला से है जो फ़ा-साद-लाम (फ-स-ल) अर्थात ف- ص- ل से है जिसमें विभाजन, अलग करना, किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच का अन्तराल या दूरी, घेरा या बाड़ा, अवरोध या सीमा, पृथक, विवरण, विस्तार, निर्णय आदि है, किन्तु मूल सेमिटिक धातु है P-S-L अर्थात पू-सादे-लम्द। ध्यान रहे प्राचीन सेमिटिक लिपियों में ‘फ’ ध्वनि नहीं थी। मज़े की बात यह कि आज अरबी लिपि में ‘प’ ध्वनि के लिए कोई चिह्न नहीं है।
P-S-L का अर्थ था पत्थर को तराशना। बात यह है कि इसका सम्बन्ध प्राचीन अरबी समाज में प्रचलित सनमपरस्ती अर्थात मूर्तिपूजा से था यानी बुत तराशना। गौर करें, प्रतिमा निर्माण के लिए पत्थर को धीरे धीरे विभाजित किया जाता है। अनघड़ पत्थर को तोड़ कर, तराशकर जो रूपाकार निर्मित होता है उस भाव का विस्तार बाद में अरबी के फ़ा-साद-लाम में मूलतः विभाजन हुआ इस कड़ी के कई शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं जैसे फ़स्ल (फसल), फ़ैसला, फ़ासला, फ़सील, तफ़सील और मुफ़स्सिल।
फस्ल का मूलार्थ है अंतर, दूरी या अंतराल। दो ऋतुओं के बीच स्पष्ट अंतराल होता है। अर्थात काल, समय या वक्त का भाव भी फस्ल में है। फस्ले बहार या फस्ले गुल का अर्थ वसंत ऋतु और फस्ले खिज़ां यानी पतझड़। फ़स्ल यानी मौसम और हर मौसम की पैदावार को मिल गया फसल का नाम। इसी तरह किसी पुस्तक के अलग-अलग अध्यायों को भी फस्ल ही कहते हैं। किसी ज़माने में दो फसलों के बीच के अंतराल में कोई भी मामला सुलझा लिया जाता था इसलिए उसे फ़ैसला कहा गया। फ़ैसला किसी उलझी बात का सुलझा हुआ, उससे अलग किया गया अंश ही होता है। अंतराल या दूरी के अर्थ में फ़स्ल से ही बना है फासला। दो फसलों के बीच का वक्त ही फासला कहलाता था। प्राचीन बस्तियां परकोटों से घिरी होती थीं जिन्हें फ़सील कहते थे। शहर और वीराने का फासला जो बताए, वही है फ़सील।
इस विवरण के बाद तफ़सील की तफ़सील स्पष्ट हुई होगी। तफ़सील में किसी कविता, कहानी पर टीक या टिप्पणी लिखना भी शामिल है। कोई फ़ेहरिस्त भी तफ़सील हो सकती है। स्पष्ट करने वाली हर क्रिया तफ़सील के दायरे में आती है। कोई भी विवरण तफ़सील या ब्योरा है। ये सारे भाव विकसित हुए हैं विभाजन करने से जो फ़साला मूलभाव है। किसी चीज़ का विभाजन दरअसल विस्तार की पहली शर्त है। यह ब्रह्माण्ड एक पिण्ड के विभाजन का परिणाम है। अन्तरिक्ष में ये पिण्ड लगातार फैल रहे हैं। विस्तार हो रहा है। यह विभाजन का परिणाम है। लिखित विवरण तब ज्यादा समझ में आते हैं जब उन्हें अलग अलग अध्यायों में समझाया जाए। गौर करें समझाना भी विस्तार का ही एक नाम है। अध्याय टुकड़ा या खण्ड ही है, जो किसी मूल पिण्ड का विभाजित हिस्सा है।
इसी तरह पश्चिमी उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में मुफ़स्सल शब्द के अनेक रूप प्रचलित हैं मसलन मुफस्सिल (यूपी-बिहार), मोफस्सल (बंगाल) और मुफशील (मराठी) इन सभी भाषाओं में मुफ़स्सल का अभिप्राय भी अन्तराल, जुड़ा हुआ, सटा हुआ या अलग किया हुआ, दूर का, विस्तार ही होता है। मुफ़स्सिल का प्रयोग आमतौर पर भौगोलिक तौर पर दूर के क्षेत्रो के लिए होता है। इसका एक अर्थ देहात भी होता है जो शहर से सटा भी हो सकता है और दूरस्थ भी। मुफ़स्सिल अदालतें यानी दूर की या शहर की परिधि से बाहर के न्यायालय। मुफ़स्सिल संवाददाता यानी देहात के रिपोर्टर या ग्रामीण संवाददाता।
ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें
|
Wednesday, February 5, 2014
अरे...अबे...क्यों बे...
हि न्दी समाज में यूँ तो ‘अबे’ सम्बोधन को हिकारत के अर्थ में लिया जाता है किन्तु इसका एक अभिप्राय निकटता जताना भी है। आमतौर पर यारी-दोस्ती और भाईचारे में अपनापा दर्शाने के लिए भी ‘अबे’ कहा जाता है। अबे से अ का लोप होकर सिर्फ ‘बे’ रह जाता है। यह भी सम्बोधन है और निकटता दरशाने के लिए प्रयुक्त होता है जैसे क्यों बे, हाँ बे, चल बे, नहीं बे आदि।
भोलानाथ तिवारी के अनुसार अबे सम्बोधनार्थी अव्यय संस्कृत के 'अयि' का रूपान्तर है। वाशि आपटे के मुताबिक यह 'अये' से आ रहा है और विस्मयबोधक अव्यय है। 'अये' में अरे का भी भाव है। कई लोगों का अरे सम्बोधन दरअसल 'अये' ही सुनाई पड़ता है। हिन्दी शब्दसागर 'अयि' रूप की बात लिखता है। हिन्दी में सही रूप 'अबे' है। हिन्दी और अन्य बोलियों में 'अबै' दरअसल अब के अर्थ में बोला जाता है। पंजाबी में ‘अबा-तबा’ भी यही है। हिन्दी में 'अबे-तुबे' करना आम मुहावरा है जिसमें बोलने वाले के अहंकार और किसी को अपमानित करने, हेयता प्रकट करने का भाव रहता है। यह जो तुबे है, अबे का अनुगामी है। अबे से दोस्ती निभाने के लिए बना लिया गया अनुकरणात्मक शब्द है।
‘अरे’ का मूल ‘आर्य’ है ऐसा कहने वाले कई नहीं ‘कुछ’ विद्वान हो सकते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो इन में भी मेरे पास सिर्फ डॉ. भगवान सिंह का हवाला ही है जिनका मानना है कि भोजपुरी का अरे तो आर्य का ही बदला हुआ रूप है। अलबत्ता साम्य के आधार पर ‘आर्ये’ से अरे का रिश्ता तार्किक नहीं लगता। संस्कृत से जितना भी थोड़ा-बहुत परिचय है उससे लगता है कि 'आर्ये' स्त्रीवाची सम्बोधन है। सिर्फ़ स्त्रीवाची सम्बोधन से ‘अरे’ अव्यय का बनना तार्किक नहीं। दूसरी बात आर्य से अज्ज > बन ही रहा है। यह तार्किक नहीं लगता कि आर्य या आर्ये से बने अरे का प्रयोग "अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, अरे नराधम" में जिस सहजता से हो रहा है वहाँ 'अरे' का आशय आर्य से रहा होगा। जबकि ‘जी’ या ‘अजी’ में जो ‘आर्य’ है उसके आधार पर कभी ऐसे वाक्यों की रचना दिखाई नहीं पड़ती, मसलन-'अजी दुष्ट, अजी मूर्ख' जैसे वाक्य नाटकीयता लाने के उद्धेश्य से या परिहास में, सायास तो कहे जा सकते हैं पर स्वाभाविक तौर पर नहीं। सो ‘अरे’ की रचना में जो आर्य है सम्बोधन उसमें निहित आदर, सम्मान का भाव वाक्य रचना में भी सुरक्षित रहेगा जैसे आर्य से बने ‘अजी’, ‘जी’ अव्यय वाले वाक्यों में यह सुरक्षित नज़र आता है।
उपरोक्त विवेचन को मेरा दुराग्रह न समझा जाए। वैसे भी अपने समय के शीर्ष विद्वान हिन्दी शब्दसागर से जुड़े थे, उसमें भी ‘अरे’ अव्यय के पीछे ‘आर्य’ सम्भावना पर विचार नहीं किया गया है। दरअसल संस्कृत के सातवें स्वर ऋ में एक सम्बोधनकारी अव्यय का भाव भी है जो स्वतंत्र रूप में ‘रे’ सम्बोधन में भी नज़र आता है और इससे ही बने ‘अरि’ में भी भद्र पुरुष का आशय है जो सम्बोधनकारक के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। आर्य से अरे की तुलना में ऋ > री > रे या अरि > अरे > रे का विकास ज्यादा तार्किक लगता है। कृ.पां. कुलकर्णी के मुताबिक सम्बोधी अव्यय अरे के मूल में अरि का एकवचन रूप काम कर रहा है जिसका संक्षेप रे भी सम्बोधी अव्यय है। प्राचीन आर्यभाषाओं में इसके ही अपभ्रंश रूप प्रयुक्त हुए हैं। कुलकर्णी यह भी बताते हैं कि संस्कृत में अरि शब्द के दो रूप है नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक अरि का मूल सुमेरी शब्दावली का एरि है जिसका अर्थ शत्रु होता है।
‘अरे’, ‘रे’ के बारे में वामन शिवराम आपटे भी संबोधनात्मक अव्यय कहते हुए इसकी व्युत्पत्ति ‘ऋ’ से बताते हैं और इसका प्रयोग अपने से छोटों को सम्बोधित करने में बताते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल क्रोध, ईर्ष्या या घृणा को व्यक्त करने में भी किया जाता है। टर्नर भी ‘अरे’ को सम्बोधी अव्यय बताते हैं। वे शतपथ ब्राह्मण का हवाला भी देते हैं। पाली, प्राकृत में भी ‘अरे’ रूप हैं। इसके अलावा उत्तर भारत की अधिकांश भाषाओं में ‘अरे’ की व्याप्ति है।
यह भी देखें- जी हुजूरिया, यसमैन, जी मैन
Thursday, May 30, 2013
ग़फ़लत में ग़ाफ़िल
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Friday, May 24, 2013
गाछ और पेड़
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Sunday, April 21, 2013
कल-कल की शब्दावली
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Saturday, April 20, 2013
‘छद्म’ और ‘छावनी’
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Monday, April 15, 2013
घोंघाबसंत
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Sunday, March 31, 2013
हथियारों के साथ ‘पंचहत्यारी’
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Tuesday, March 5, 2013
बर्ताव, आचरण और व्यवहार
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Monday, February 25, 2013
क़िस्सा दक़ियानूस का
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
प्रस्तुतकर्ता
अजित वडनेरकर
5
कमेंट्स
पर
5:18 PM
![]() लेबल:
god and saints,
shelter,
इतिहास,
इस्लाम islam,
पद उपाधि,
व्यवहार,
सम्बोधन,
स्थान
लेबल:
god and saints,
shelter,
इतिहास,
इस्लाम islam,
पद उपाधि,
व्यवहार,
सम्बोधन,
स्थान
Saturday, February 9, 2013
होशियारी की बातें
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Tuesday, January 15, 2013
चर्चा कैसी कैसी !!
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |

![Sachin-Tendulkar[5] Sachin-Tendulkar[5]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs-gf4vc4NGDrd7qPVBZ6tK_SpQQ8Tnn4vlrDCwWL3mossMB0CZxqCaHT2sBg6erhzFj_T3te8tScn_nwJXNbMlm-rdCZL5eU8KmLmiZcJ4660MfXoZQopPtMmUJvLCPyDcKzxrUPMntw4/?imgmax=800)