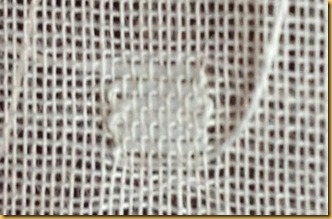पूर्णता में ही 'कमाल'
यह जो पूर्णता है बड़ी चमत्कारी है। किसी चीज़ के पूरा होने का अहसास हमें गहरी शान्ति से भर देता है। पूर्णता सुख का सर्जन करती है और आगे बढ़ने का रास्ता खोलती है। हमारे हाथों उस चमत्कारी भविष्य की नींव रखी जाती है जिसके लिए हमने ईश्वर का आविष्कार किया था। ज्ञानियों ने इस कर्मयोग को ही ईश्वरोपासना कह दिया। बहरहाल पूर्णता में ही ‘कमाल’ है।
उपज्यो पूत 'कमाल'
अरबी से फ़ारसी होते हुए हिन्दी में आए कमाल के डीएनए में इसी पूर्णता का भाव है। कबीर ताउम्र इन्सानियत की बात करते रहे। वे सन्त थे। ज्ञानमार्गी थे जिसका मक़सद सम्पूर्णता की खोज था। आख़िर क्यों न वे अपने पुत्र का नाम कमाल रखते ! कमाल अपने पूरे कुनबे के साथ उर्दू में है और कुछ संगी साथी हिन्दी में भी नज़र आते हैं। कमाल کمال बना है अरबी की मूलक्रिया कमल کمل से जो मूलतः क-म-ल है, अर्थात काफ़(ک) मीम( م ) लाम (ل) से जिसमें पूर्ण होने, पूर्ण करने का भाव है।
'कमाल' का चमत्कार
इस तरह कमाल में परम, सम्पूर्णता, सिद्धि, पराकाष्ठा, सर्वोत्कृष्टता जैसे भाव स्थापित हुए हिन्दी में कमाल का बर्ताव चमत्कारी, अद्भुत या आश्चर्यजनक के अर्थ में ज्यादा होता है। जबकि इसका मूल भाव Completion, perfection या entire है। जब कोई चीज़ अपनी सम्पूर्णता में रची जाती है या घटित होती है तब सामान्य मनुष्य के लिए वह आश्चर्य ही होता है। इसीलिए सम्पूर्ण उपलब्धि को हम अनोखापन मानते हैं।
'कमाल' के मुहावरे
हिन्दी में कमाल दिखाना, कमाल करना, कमाल है जैसे मुहावरे हमारी रोज़मर्रा की अभिव्यक्ति का हिस्सा हैं। इनके बिना काम नहीं चलता। कमाल शब्द ग्रामीण बोली से लेकर शहरी ज़बान में छाया हुआ है। “कमाल की चीज़’, ‘कमाल की बात”, “कमाल की एक्टिंग”, “कमाल की सोच”, “कमाल की तकनीक”, “कमाल का हुनर”, “कमाल का आदमी”, “कमाल की औरत” जैसे दर्जनों पद हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं जिसमें कमाल का अर्थ या तो प्रवीणता, पराकाष्ठा है अन्यथा आश्चर्य का भाव है।
'कमाल' का कुटुम्ब
कमाल-कुटुम्ब का ही एक अन्य शब्द है जो सम्पूर्णता के अर्थ में हिन्दी में प्रतिष्ठित है वह है مکمل मुकम्मल। कुछ लोग मुकम्मिल भी लिखते हैं। अनेक लोग मुक्कमल लिख देते हैं। सही मुकम्मल है अर्थात मीम काफ मीम लाम। मुकम्मल बना है कमाल से पहले ‘मु’ उपसर्ग लगने से जो मूलतः सम्बन्धकारक है।
'कमाल' यानी सम्पूर्णता
जिसमें सम्पूर्णता का गुण है उसका अर्थ होगा सम्पूर्ण। सो मुकम्मल में सम्पूर्ण, सर्वोत्कृष्टता जैसे भाव हैं। मुकम्मल वह है जो परिपूर्ण है, निर्मित है, बना हुआ है। वह जिसमें कुछ भी करने को शेष न रह गया हो। इसी कड़ी में आता है कामिल کامل इसमें भी यही सारे भाव समाहित हैं। कामिल अरबी की प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुरुषवाची संज्ञा भी है। अखिल,योग्य, परिपूर्ण, सम्पूर्ण, सक्षम जैसी अर्थवत्ता इसमें है।
नामों में 'कमाल'
इसी तरह ताकमाल, मुकतामिल, ताकमुल, ताकमिल, कमालान जैसे पुरुषवाची नाम हैं तो कामिलात, कामिलिया, कमिल्ला जैसे स्त्रीवाची नाम भी इसी मूल से निकले हैं जिनमें उपरोक्त भाव ही हैं। इस कड़ी के ये सभी शब्त अरबी, फ़ारसी, हिन्दी, तुर्की, अज़रबैजानी, स्वाहिली, इंडोनेशियाई आदि अनेक भाषाओं में इस्तेमाल होते हैं। हिन्दी के अलावा अनेक भारतीय भाषाओं में भी इस शृंखला के शब्द हैं।
ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें
|