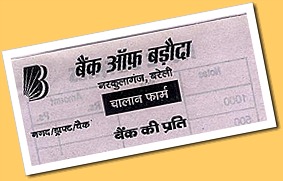ग र्मागर्म पूरियों में बेड़मी पूरी (या कचौरी) लाजवाब होती है। अपनी मनपसंद निहारी है ये। आगरा में इसे बेड़ई कहा जाता है। हींग के धमार वाली आलू की गाढ़ी-गाढ़ी तरकारी से भरे दोने में डूबी बेड़मी पूरी से सुबह जायकेदार हो जाती है। कभी सोचा न था कि इस बेड़मी/बेड़ई का रिश्ता हथकड़ी वाली बेड़ी से भी होगा और ग़र्क़ होने वाले बेड़े/बेड़ा से भी होगा। बेड़िया और बेड़नी से भी होगा जिन्हें नट/घुमन्तू जाति माना जाता है। जानते हैं इन शब्दों के दिलचस्प सफर को।
अलग-अलग अर्थछटाओं वाले इन शब्दों में कैसी रिश्तेदारी? बात दरअसल यह है कि इन सभी में कहीं न कहीं घूमने, घेरने, पूरने, समाने का भाव है किन्तु इस पर आसानी से ध्यान नहीं जाता। वैदिक साहित्य में एक शब्द है वेष्ट जिसमें लपेटना, लिपटाना, बान्धना, घुमाव, आवरण, भरना, आवृत्त करना जैसे भाव हैं। डॉ रामविलास शर्मा के मुताबिक संस्कृत वेष्ट का ही प्राकृत प्रतिरूप विष्ट है। मुझे लगता है कि विष्ट और वेष्ट एक ही मूल से ज़रूर उपजे हैं पर विष्ट प्राकृत रूप नहीं है। हाँ, इन्हें एक दूसरे का प्रतिरूप भी माना जा सकता है। विष्ट का प्राकृत रूप विट्ठ होता है, जबकि डॉ. रामविलास शर्मा इसे ही प्राकृत का बता रहे हैं। इसकी पुष्टि प्राकृत शब्दकोश ‘पाइय सद्द महण्णवो’ से भी होती है जिसमें विष्ट का प्राकृत रूप विट्ठ बताया गया है। बात यूँ है कि मूल रूप विष्ट है, इसका विकास वेष्ट है।
जो भी हो, संस्कृत में भी एक ही शब्द के अनेक रूप प्रचलित है यह कई बार साबित होता है। इसी तरह संस्कृत शब्दावली में भी प्राकृत शब्द जस के तस या थोड़े बहुत फेरबदल के साथ मिलते हैं। विष्ट का प्राकृत रूप विट्ठ भी होता है, विड्ड भी और विड्ढ भी। विष्ट के मूल में विष् / विश् धातु है जिसमें समष्टि का भाव है। विश्व यानी संसार भी इसी शब्द से बना है और विष्णु भी। विश् धातु में समाना, दाखिल होना, प्रविष्ट होना जैसे भाव हैं। समाविष्ट पर गौर करें। इससे बने विश्व का अर्थ है सारा, सब कुछ, सार्वलौकिक, सार्वकालिक, सृष्टि, प्रत्येक आदि। विश्व शब्द में जो भाव है वह प्रकृति को ईश्वर मानने के सार्वकालिक मानव दर्शन की ही पुष्टि करता है। समस्त धर्मशास्त्रों में जिस परम् की बात कही जाती है उसी ब्रह्म का व्यक्त रूप विश्व है। जिस तरह शरीर की आत्मा नजर नहीं आती, शरीर नजर आता है, उसी तरह विश्वात्मा यानी ब्रह्म का लौकिक स्वरूप ही विश्व है। बहरहाल, इसी विश् से विकसित विष्ट में घेरने, समाने के भाव भी उजागर हुए। विष्ट का प्राकृत रूप विट्ठ है। पंढरपुर के प्रसिद्ध लोकदेवता विट्ठल इसका अगला रूप हुआ। संस्कृत में विट्ठल का विड्ढल रूपान्तर भी विद्यमान है। ध्यान रहे, विट्ठल में विष्णु का रूप देखा जाता है। विष्णु का मूल भी विष् / विश् है।
स्पष्ट है कि जिस तरह विष्ट से विड्ड और विड्ढ बन रहा है उसे तरह वेष्ट से वेड्ड, वेड्ढ और वेढ भी बनता है। भाव वही- समाना, पूरना, घेरना, आवृत्त करना आदि। वेढ से वेढम का विकास हुआ और फिर इसस बना वेढमिका। वेढ़मिका का सबसे पहला उल्लेख अमरकोश में मिलता है। इसके आधार पर मोनियर विलियम्स ने संस्कृत कोश में वेढमिका की प्रविष्टि दर्ज है- “a kind of bread or cake” इसी तरह रॉल्फ़ लिली टर्नर इसमें जोड़ते हैं- “cake of flour mixed or filled with pulse or meal” जाहिर है आशय पूरी या कचौरी से है। हिन्दी शब्दसागर में वेढमिका का अर्थ “वह कचौरी जिसमें उड़द की पीठी भरी हुई हो” बताया गया है। इसमें व्युत्पत्ति संस्कृत वेढग से बताई गई है पर इसका अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता। वेढमिका से बेड़ई या बेड़मी बनने का विकासक्रम कुछ यूँ रहा- वेढमिका > वेडइआ > बेड़ई> अथवा वेढमिका > वेढमिआ > बेड़मी। वेष्ट में निहित समाने, भरने, पूरने, घेरने, ढकने, आवृत्त करने जैसे अर्थ पूरी, कचौरी बनाने की प्रक्रिया में सार्थक हो रहे हैं। पूरी नाम ही पूरने से पड़ा है। जिसमें कुछ पूरा जाए, भरा जाए यानी स्टफिंग की जाए। आटे की गोल गोल लिट्टी में किस तरह छोटा गढ़ा बनाया जाता है। स्वादिष्ट मसाला उसमें समा जाता है। फिर मसाले पर आवरण चढ़ा दिया जाता है और लिट्टी को गोल गोल बेल कर या हाथों से चपटा कर तेल / घी में तल लिया जाता है। अब आते हैं बेड़ा पर। आमतौर पर बेड़ा शब्द वाहनों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है किन्तु इसका आशय जहाजों के समूह से है। हालाँकि बेड़ा शब्द का मूल अर्थ है पोत, जहाज़ या बड़ी नौका। यह बेड़ा शब्द भी वेष्ट > वेड्ढ > बेड़ > से विकसित हुआ है। बेड़ क्रिया में बान्धने, लपेटने का भाव किसी भी बेड़े के निर्माण की प्रक्रिया से समझा जा सकता है। प्राचीनकाल में बेड़े का निर्माण लकड़ी के बड़े बड़े फट्टों को आपस में बांध कर किया जाता था। इन तख़्तों पर पुआल बिछा कर सफर किया जाता था। इस तरह बेड़े में जो अर्थवत्ता उभर रही है वह तख्तों को आपस में बान्धने, रस्सी लपेटने और उन्हें घेरने में निहित है। बाद में लकड़ी के फट्टों के स्थान पर कई नावों को बांध कर एक बेड़ा बनाया जाने लगा जिस पर लकड़ी के फट्टे डाल कर उस पर भारी सामान ढोया जाता था। नावों के इसी समूह की वजह से फ्लीट के अर्थ में बेड़ा शब्द रूढ़ हुआ। बेड़ा का एक रूप भेड़ा भी है जैसे जबलपुर के पास नर्मदा तट पर भेड़ाघाट अर्थात वह स्थान जहाँ से नावें चलती हों। प्राचीनकाल मे जलमार्ग भी आवागमन का महत्वपूर्ण जरिया था। ये सफर बेहद कठिन होता था इसीलिए “बेड़ा पार” होने का भाव कठिनाई पर विजय पाने जितना महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। “बेड़ा ग़र्क़” में विपत्ति या विनाश का भाव समझा जा सकता है। प्राचीन ग्रन्थों में बेड़ी, वेड़ी, वेटी, बेडा जैसे शब्दों में कश्ती या नौका का भाव है। इसमें वाहन में निहित घूमाव, भ्रमण, गति जैसे भाव तो हैं ही, बान्धने, लपेटने जैसी क्रियाओं की वजह से भी इसका नाम सार्थक हो रहा है।
बुंदेलखण्ड क्षेत्र में विमुक्त और घुमन्तू बेड़िया जाति होती है। इस जाति की स्त्रियाँ कमाल कुशल नृत्यांगना होती हैं। इन्हें बेड़नी कहते हैं। बुंदेलखण्ड के प्रसिद्ध राई नृत्य में ये बेड़नियाँ निष्णात होती हैं। अपनी अनथक अनवरत चक्रगति की वजह से राई नृत्य भारतीय लोकविधाओं में अन्यतम है। बेड़िया शब्द में भी वेड क्रिया की गति, घुमाव स्पष्ट हो रहा है। डॉ. रामविलास शर्मा के मुताबिक बांग्ला में बेड़ घुमाव का अर्थ देता है। बेड़ी शब्द का रिश्ता किन्ही कोशों में वलय से जोड़ा जाता है जो बेड़, वेड क्रियाओं की इतनी स्पष्ट व्याख्या के बाद उचित नहीं जान पड़ता। हमारा मानना है कि हथकड़ी या बन्धन के तौर पर प्रयुक्त बेड़ी शब्द वेष्ट से विकसित बेड़ क्रिया से ही आ रहा है। बेड़ी जो बान्धने के काम आती है। बेड़ा इसलिए जिसे बान्धा गया है। बान्धने में घुमाने की क्रिया है। बेड़नी घूमती है। बेड़िया घूमते हैं। बेड़ा घूमता है। बेड़ई में मसाला समाविष्ट है। बेड़मी कचौरी एक आवरण है। इसे गोल गोल बनाया जाता है। गोल बनाने के लिए लिट्टी को घुमाया जाता है। | ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
अभी और बाकी है। दिलचस्प विवरण पढ़ें आगे...
![]() लेबल:
food drink,
पदार्थ
लेबल:
food drink,
पदार्थ