| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Monday, April 3, 2023
‘नाबाद’ के बहाने ‘बाद’ की बातें
प्रस्तुतकर्ता
अजित वडनेरकर
15
कमेंट्स
पर
12:41 PM
![]() लेबल:
तकनीक,
व्यवहार
लेबल:
तकनीक,
व्यवहार
Tuesday, September 20, 2016
बालों की दवाई, शिकाकाई, कहाँ से आई...
सिगा, सिगाई और जूड़ा
जानते हैं शिकाकाई शब्द की जन्मकुण्डली। जब पढ़ते थे तब शिकाकाई शब्द जापानी भाषा का लगता था। पिछली बार जब सोलापुर गए तो इस सन्दर्भ में कुछ बातें पता चली थीं। वहाँ के पुराने बाज़ार में तरह-तरह की जड़ीबूटियाँ बिक रही थीं। कुछ दवाओं और तेल आदि के विज्ञापनों में बालों का जूड़ा प्रदर्शित था। सोलापुर का आन्ध्रप्रदेश से गहरा सम्बन्ध है। वहाँ तेलुगुभाषी बहुतायत रहते हैं। बहरहाल, एक ऐसी दुकान पर भी पहुँचे जहाँ विशुद्ध रूप से बालों की देखभाल वाली जड़ीबूटियाँ ही थीं। वहाँ जूड़े के लिए अनेक लोगों के मुँह से ‘सिगा’ अथवा ‘सिगाई’ शब्द सुना।
शिखण्डी से रिश्तेदारी
जब उन्हें बताया कि मैं मराठी हूँ तो दुकानदार ने सिर की तरफ़ इशारा किया, शेंडी शेंडी। मराठी में शेंडी का अर्थ होता है जूड़ा या सिर के बीच लपेट कर रखी चुटिया। शेंडी बना है शिखण्डिका से। शिख+ अण्ड में शिखण्ड यानी जूड़े का भाव है। शिख यानी सिर के सबसे ऊँचे हिस्से पर बालों से बनाया अण्डाकार गुच्छा यानी शिखण्ड। संस्कृत में इसके लिए चूड़ा शब्द भी है। चूड़ाकरण का अर्थ मुण्डन भी होता है। चूड़ा का ही अगला रूप जूड़ा है।
सिका, सिकु, सिक्कम्
बहरहाल, शिखण्डिका के शिख या शिखा से अचानक तेलुगू का ‘सिगा’ पकड़ में आ गया जो अन्यथा नहीं आता। चार्ल्स फिलिप ब्राऊन के तेलुगू कोश में सिगा और सिका दोनों की प्रविष्टि है और उसका अर्थ जूड़ा, चोटीगुच्छ, चूड़ा या शिखा आदि ही बताया गया है। तमिळ लैक्सिकन में इसके कई रूप प्रचलित हैं जैसे- सिका, सिक्कु, सिक्कम्, सिकाईताटू, सिकरिन, सिकुरम आदि। इनके संस्कृत रूपान्तर की कल्पना की जा सकती है मसलन शिखा, शिखु, शिखरम्, शिखरिणी आदि। द्रविड़ भाषाओँ में संस्कृत की तत्सम शब्दावली के नितान्त देसी रूप इस तरह घुले-मिले हैं कि यह कहना कठिन है कि संस्कृत ने द्रविड़ को प्रभावित किया है द्रविड़ ने संस्कृत को।
काई यानी फल, सिका यानी शिखा
गौरतलब है कि तमिल में काई यानी kay फल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अनेक सन्दर्भों में इसका अर्थ कच्चा फल, सूखा फल भी दिया गया है। तो सिका-काई का अर्थ हुआ शिखा- काई अर्थात चूड़ा-फल या शिखाफल। ज़ाहिर है कि इस नामकरण के पीछे बालों के काम आने वाला फल से ही तात्पर्य है। शिकाकाई का वानस्पतिक नाम अकेशिया कोनसिन्ना है।
शेखर और शिखरिणी
शिकाकाई ज्यादातर गर्म जलवायु में पैदा होने वाली झाड़ी है। इसका तेल भी बनाया जाता है और इसे पीस कर विभिन्न प्रकार की ओषधियाँ भी बनाई जाती हैं। ध्यान रहे, शिव को शेखर कहते हैं क्योंकि वे सिर पर जटा बान्धते हैं। इसका रिश्ता गंगा से है। इसीलिए उसका नाम शिखरिणी भी है। पूर्वांचल के लोग अपने नाम के साथ शेखर लगाना पसंद करते हैं।
देखें फेसबुक पर शिकाकाई
ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें
|
Saturday, August 6, 2016
कुछ ‘दन्द-फन्द’ कर लिया जाए
दन्द यानी जोड़ा या जद्दोजहद
संस्कृत क्रियामूल द्व / द्वि में दो का आशय है और द्वन्द्व इससे ही बना है जिसका का अर्थ है संग्राम, लड़ाई, झगड़ा, हाथापाई, संघर्ष वग़ैरह। इसमें दो का भाव साफ़ नज़र आ रहा है। हिन्दी का दो भी द्व से ही बना है। द्वक, द्वय, द्वन्द्व, जैसे शब्दों में दो और दो, सम्मुख, जोड़ा, युगल, जद्दोजहद, परस्पर, स्पर्धा, होड़, तकरार, अनबन, आज़माइश जैसे भाव हैं। यही नहीं, मूलतः द्वन्द्व में परस्पर विपरीत जोड़ी का आशय भी है इसलिए इसका अर्थ स्त्री-पुरुष युगल भी है। व्याकरण में द्वन्द्व समास होता है। समास युग्मपद है। परस्पर विलोम या विपरीतार्थी शब्द भी द्वन्द्व की मिसाल है मसलन सुख-दुख, रात-दिन वगैरह।
फन्द यानी गिरह
दंद की तर्ज़ फर फंद का इसमें जोड़ा जाना लोकअभिव्यक्ति की सफलता है। भाषा ऐसे पदों से ही समृद्ध होती है। यह जो फंद है, यह दन्द का अनुकरणात्मक पद न होते हुए स्वतन्त्र शब्द है जो ‘फंदा’ वाली शृंखला से आ रहा है। फन्द यानी बन्धन या पाश। देवनागरी में प > फ > ब > भ की शृंखला के शब्द स्थानीय प्रभाव के चलते विभिन्न बोलियों में एकदूसरे की जगह लेते हैं। बन्ध का लोकरूप फन्द हो जाता है। बन्ध में जहाँ किसी भी किस्म के अवरोध, रोक, गिरह या गाँठ का भाव है वहीं फन्दा सिर्फ़ गाँठ है। बान्धने की क्रिया सिर्फ़ गाँठ से ही व्यक्त नहीं होती। पानी को रोकने वाली व्यवस्था बान्ध इसलिए कहलाती है क्योंकि उसे बान्ध दिया गया है। फन्दा भी एक किस्म का बन्धन है पर हर बन्धन फन्दा नहीं। अलबत्ता फन्दा जहाँ गाँठ है वही इसी तर्ज़ पर बन्धा गाँठ न होकर डैम या बान्ध को कहते हैं।
जी-तोड़ प्रपंच
अब दंद-फंद की बात। मूल रूप से अपने मक़सद की कामयाबी के लिए हर मुमकिन और हर तरह के प्रयासों को अभिव्यक्त करने वाला पद है दंद-फंद पर अब इसका प्रयोग नकारात्मक अर्थ में ही ज़्यादा होता है। आज की हिन्दी में इस पद में चालबाजी, षड्यन्त्र, हथकण्डा, दाँव-पेच, खटराग, कूटनीति जैसी अभिव्यक्तियाँ समा गई हैं। द्वन्द्व से बने दन्द से यहाँ ज़ोर-आज़माइश प्रमुख है वहीं फन्द में फँसाने का भाव है। कुल मिला कर उचित-अनुचित का विचार किए बिना उद्धेश्यपूर्ति का प्रयत्न दरअल दंद-फंद की श्रेणी में आता है। हालाँकि सामान्य तौर पर जी-तोड़ मेहनत के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है जैसे- “सारे दन्द-फन्द कर लिए, तब कहीं काम मिला” या “वहाँ किराए के मकान के लिए बड़े दन्द-फन्द करने पड़ते हैं” वगैरा वगैरा।
दन्दाँ तुर्श करदन
जिस तरह संस्कृत में विसर्ग का उच्चार ‘ह’ होता है पर अक्सर वह ‘आ’ में परिवर्तित हो जाता है। फ़ारसी में शब्द के अन्त में ‘हे’ का प्रयोग इसी तरह होता है। संस्कृत के दन्त यानी दाँत का फ़ारसी समानार्थी दंदानह دندانه है जो दाल, नून, दाल,अलिफ़, नून, हे से मिलकर बना है। हिन्दी में इसका उच्चार दंदाना होता है जिसका अर्थ हुआ दाँता, दाँतेदार, नुकीला, नोकदार आदि। फ़ारसी में कहावत है “दन्दाँ तुर्श करदन” इसकी तर्ज़ पर हिन्दी में दाँत खट्टे करना कहावत बनाई गई। दन्द-फन्द वाले दन्द से दाँतेदार दन्द का कुछ लेना-देना नहीं।
ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें
|
Saturday, April 20, 2013
‘छद्म’ और ‘छावनी’
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Sunday, March 31, 2013
हथियारों के साथ ‘पंचहत्यारी’
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Tuesday, January 29, 2013
महिमा मरम्मत की
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Friday, January 4, 2013
अहाते में…
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Wednesday, January 2, 2013
क़िस्त दर क़िस्त…

हिन्दी में किस्त का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रयोग कई हिस्सों में भुगतान के लिए होता है । आजकल इसके लिए इन्स्टॉलमेंट या इएमआई शब्द भी प्रचलित हैं मगर किस्त कहीं ज्यादा व्यापक है । भुगतान-संदर्भ के अलावा मोहम्मद मुस्तफ़ा खाँ मद्दाह के उर्दू-हिन्दी कोश के अनुसार किस्त में सामान्य तौर पर किसी भी चीज़ का अंश, हिस्सा, टुकड़ा, portion या भाग का आशय है । अरबी कोशों में अंश, हिस्सा, पैमाना, पानी का जार या न्याय जैसे अर्थ मिलते हैं । न्याय में निहित समता और माप में निहित तौल का भाव किस्त में है और इसीलिए कहीं कहीं किस्त का अर्थ न्यायदण्ड या तुलादण्ड भी मिलता है ।
सबसे पहले क़िस्त के मूल की बात । अरबी कोशों में क़िस्त को अरबी का बताया जाता है जिसकी धातु क़ाफ़-सीन-ता (ق س ط) है । हालाँकि अधिकांश भाषाविद् अरबी क़िस्त का मूल ग्रीक ज़बान के ख़ेस्तेस से मानते हैं जिसका अर्थ है माप या पैमाना । लैटिन ( प्राचीन रोम ) में यह सेक्सटैरियस (Sextarius) है । ग्रीक ज़बान का ख़ेस्तेस, लैटिन के सेक्सटैरियस का बिगड़ा रूप है । यूँ ग्रीक भाषा लैटिन से ज्यादा पुरानी मानी जाती है मगर भाषाविदों का कहना है कि सेक्सटैरियस रोमन माप प्रणाली से जुड़ा शब्द है । यह माप पदार्थ के द्रव तथा ठोस दोनों रूपों की है । सेक्सटेरियस दरअसल माप की वह ईकाई है जिसमें किसी भी वस्तु के 1/6 भाग का आशय है । समूचे मेडिटरेनियन क्षेत्र में मोरक्को से लेकर मिस्र तक और एशियाई क्षेत्र में तुर्की से लेकर पूर्व के तुर्कमेनिस्तान तक ग्रीकोरोमन सभ्यता का प्रभाव पड़ा । खुद ग्रीक और रोमन सभ्यताओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया इसीलिए यह नाम मिला ।
सेक्सटैरियस में निहित ‘छठा भाग’ महत्वपूर्ण है जिसमें हिस्सा या अंश का भाव तो है ही साथ ही इसका छह भी खास है । दिलचस्प है कि सेक्सटैरियस में जो छह का भाव है वह दरअसल भारोपीय धातु सेक्स (seks ) से आ रहा है । भाषाविदों का मानना है कि संस्कृत के षष् रूप से छह और षष्ट रूप से छट जैसे शब्द बने । अवेस्ता में इसका रूप क्षवश हुआ और फिर फ़ारसी में यह शेश हो गया । ग्रीक में यह हेक्स हुआ तो लैटिन में सेक्स, स्लोवानी में सेस्टी और लिथुआनी में सेसी हुआ । आइरिश में यह छे की तरह ‘से’ है । अंग्रेजी के सिक्स का विकास जर्मनिक के सेच्स sechs से हुआ है । सेक्सटैरियस का बिगड़ा रूप ही ग्रीक में खेस्तेस हुआ । खेस्तेस की आमद सबसे पहले मिस्र मे हुई।
समझा जा सकता है कि इसका अरब भूमि पर प्रवेश इस्लाम के जन्म से सदियों पहले हो चुका था क्योंकि अरब सभ्यता में माप की इकाई को रूप में क़िस्त का विविधआयामी प्रयोग होता है । यह किसी भी तरह की मात्रा के लिए इस्तेमाल होता है चाहे स्थान व समय की पैमाईश हो या ठोस अथवा तरल पदार्थ । हाँ, प्राचीनकाल से आज तक क़िस्त शब्द में निहित मान इतने भिन्न हैं कि सबका उल्लेख करना ग़ैरज़रूरी है । खास यही कि मूलतः इसमें भी किसी पदार्थ के 1/6 का भाव है जैसा कि पुराने संदर्भ कहते हैं । आज के अर्थ वही हैं जो हिन्दी-उर्दू में प्रचलित हैं जैसे फ्रान्सिस जोसेफ़ स्टैंगस के कोश के अनुसार इसमें न्याय, सही भार और माप, परिमाप, हिस्सा, अंश, भाग, वेतन, किराया, पेंशन, दर, अन्तर, संलन, संतुलन, समता जैसे अर्थ भी समाए हैं । क़िस्त में न्याय का आशय भी अंश या भाग का अर्थ विस्तार है । कोई भी बँटवारा समान होना चाहिए । यहाँ समान का अर्थ 50:50 नहीं है बल्कि ऐसा तौल जो दोनों पक्षों को ‘सम’ यानी उचित लगे । यह जो बँटवारा है , वही न्याय है । इसे ही संतुलन कहते हैं और इसीलिए न्याय का प्रतीक तराजू है ।
जहाँ तक क़िस्त के किश्त उच्चार का सवाल है यह अशुद्ध वर्तनी और मुखसुख का मामला है । वैसे मद्दाह के उर्दू-हिन्दी कोश में किश्त का अलग से इन्द्राज़ है । किश्त मूलतः काश्त का ही एक अन्य रूप है जिसका अर्थ है कृषि भूमि, जोती गई ज़मीन आदि । काश्तकार की तरह किश्तकार का अर्थ है किसान और किश्तकारी का अर्थ है खेती-किसानी । किश्तः या किश्ता का अर्थ होता है वे फल जिनसे बीज निकालने के बाद उन्हें सुखा लिया गया हो । सभी मेवे इसके अन्तर्गत आते हैं । किश्त और काश्त इंडो-ईरानी भाषा परिवार का शब्द है । फ़ारसी के कश से इसका रिश्ता है जिसमें आकर्षण, खिंचाव जैसे भाव हैं । काश्त या किश्त में यही कश है । गौर करें ज़मीन को जोतना दरअसल हल खींचने की क्रिया है । कर्षण यानी खींचना । आकर्षण यानी खिंचाव । फ़ारसी में कश से ही कशिश बनता है जिसका अर्थ आकर्षण ही है ।
ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें
|
प्रस्तुतकर्ता
अजित वडनेरकर
11
कमेंट्स
पर
10:24 PM
![]() लेबल:
business money,
government,
उपकरण,
काल समय,
खेती,
तकनीक,
माप तौल,
व्यवहार
लेबल:
business money,
government,
उपकरण,
काल समय,
खेती,
तकनीक,
माप तौल,
व्यवहार
Sunday, December 9, 2012
सुरख़ाब के पर
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
प्रस्तुतकर्ता
अजित वडनेरकर
10
कमेंट्स
पर
9:03 PM
![]() लेबल:
animals birds,
nature,
चमक,
तकनीक,
पद उपाधि,
व्यवहार
लेबल:
animals birds,
nature,
चमक,
तकनीक,
पद उपाधि,
व्यवहार
Monday, October 29, 2012
रफूगरी, रफादफा, हाजत-रफा
पिछली कड़ियाँ- 1.‘बुनना’ है जीवन.2.उम्र की इमारत.3.‘समय’ की पहचान.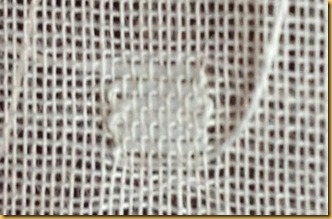
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Saturday, October 27, 2012
‘दफा’ हो जाओ …
 1.‘बुनना’ है जीवन.2.उम्र की इमारत.3.‘समय’ की पहचान.
1.‘बुनना’ है जीवन.2.उम्र की इमारत.3.‘समय’ की पहचान.
ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें
|
प्रस्तुतकर्ता
अजित वडनेरकर
3
कमेंट्स
पर
10:27 PM
![]() लेबल:
animals birds,
government,
nature,
काल समय,
तकनीक,
व्यवहार,
सेना,
स्थिति
लेबल:
animals birds,
government,
nature,
काल समय,
तकनीक,
व्यवहार,
सेना,
स्थिति
Monday, October 22, 2012
‘बुनना’ है जीवन
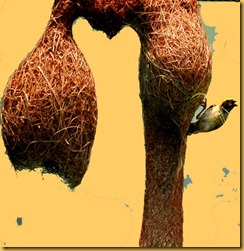
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Tuesday, September 25, 2012
‘वापसी’ का भेद
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
Wednesday, August 22, 2012
‘मा’, ‘माया’, ‘सरमाया’ [माया-2]

| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |
प्रस्तुतकर्ता
अजित वडनेरकर
4
कमेंट्स
पर
1:38 PM
![]() लेबल:
business money,
government,
nature,
space astronomy,
खेती,
चमक,
तकनीक,
राजनीति,
विज्ञान,
व्यवहार
लेबल:
business money,
government,
nature,
space astronomy,
खेती,
चमक,
तकनीक,
राजनीति,
विज्ञान,
व्यवहार
Wednesday, August 8, 2012
जासूस की जासूसी
| ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें |

![Sachin-Tendulkar[5] Sachin-Tendulkar[5]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs-gf4vc4NGDrd7qPVBZ6tK_SpQQ8Tnn4vlrDCwWL3mossMB0CZxqCaHT2sBg6erhzFj_T3te8tScn_nwJXNbMlm-rdCZL5eU8KmLmiZcJ4660MfXoZQopPtMmUJvLCPyDcKzxrUPMntw4/?imgmax=800)


























































