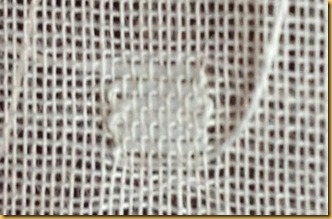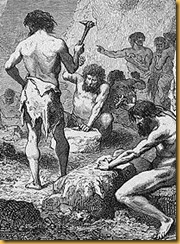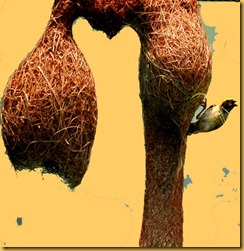यह जानना बेहद जरूरी है कि सवालिया निशान के दायरे में जितने भी सवाल हैं, पूरी दुनिया में ‘क’ से ही अभिव्यक्त होते हैं। इसे अंग्रेजी में 5W & 1H अथवा “पंचवकार, एक हकार” कहा जाता है। हिन्दी में ‘ककारषष्ठी’ कहा जा सकता है। यह दिलचस्प है कि संस्कृत के किम् में एक साथ तमाम प्रश्नवाची जिज्ञासाएँ समाई हुई है अर्थात क्या, क्यों, कब, कहाँ आदि...। इस किम से ही हिन्दी के तमाम प्रश्नवाची सर्वनामों यानी ‘कौन’, ‘कब’, ‘कहाँ’, ‘क्या’, ‘कैसे’, ‘किस’ आदि पैदा हुए हैं। इनमें सबका अपना-अपना महत्व है। कोई भी मानवीय जिज्ञासा इन सवालों के बिना पूरी नहीं होती। कोई भी कथा तब तक पूरी नहीं होती जब तक इस ‘ककारषष्ठी’ का समावेश उसमें न कर दिया जाए।
पत्रकारिता में तो इन शब्दों का महत्व गीता-कुरान-बाइबल से भी ज्यादा है। किसी भी घटना/ वारदात/ प्रसंग को जब तक इन कब-क्यों से न गुज़ारा जाए, उसे खबर की शक्ल में ढाला नहीं जा सकता। अफ़सोस कि आज के पत्रकार खबर लिखने से पहले ‘ककारषष्ठी’ मन्त्र का आह्वान नहीं करते। शायद शर्म आती होगी तो ‘6K’ की तरह याद कर लें, इसे भूल कर कोई खबर बन नहीं सकती और आप साख कमा नहीं सकते।
तो ‘किम्’ से जन्में ‘क्यों ‘का ही एक रूप है ‘चूँ’ जिसमें सवाल छिपे हैं। ध्यान रहे कि बच्चे ‘क’ और ‘च’ ध्वनियाँ सहज रूप से उच्चार लेते हैं मगर संयुक्त ध्वनियों का उच्चार नहीं कर पाते। यह समस्या अनेक मानव समूहों में भी होती है। नासिक्य स्पर्श के साथ क+य से बने क्यों का रूपान्तर ‘चों’ जाता है। अनेक लोग इसी प्रश्नवाचक चों को उच्चारते हैं। ‘क्यों’ का एक रूप फ़ारसी-उर्दू में ‘क्यूँ’ हो जाता है। स्वाभाविक है कि ‘क्यों’ से ‘चों’ की तरह ‘क्यूँ’ से ‘चूँ’ भी बन जाता है।
अब ‘क्यूँ’ हो या ‘चूँ’, है तो सवाल ही। ...और हमारा समाज जवाबदेही से हमेशा बचता नज़र आता है। भाषाओं के विकास में ही मानव-विकास नज़र आता है। लोकतन्त्र विरोधी समाज ही सवालों से कतराता है। “ज्यादा चूँ-चपड़ की तो...” एकाधिकारवादी, सामन्तवादी और सवालों से कतराते समाज की अभिव्यक्ति है। इसमें यह निहित है कि ज्यादा सवाल पूछेंगे, तो ख़ैर नहीं।
इस तब्सरे के बाद यह समझना मुश्किल नहीं बात बात में बोला जाने वाला अव्यय ‘चूँकि’ यूँ तो फ़ारसी का है पर ‘क्यूँकि’ का ही रूपान्तर है। हालाँकि जॉन प्लॉट्स ‘चूँ’ को फ़ारसी के ‘चिगुन’ से व्युत्पन्न मानते हैं जिसमें क्यों, कहाँ, कैसे का भाव है। सवाल यह है कि जब फ़ारसी में स्वतन्त्र रूप में ‘चि’ अव्यय मौजूद है और उसमें भी वही प्रश्नवाची आशय मौजूद है तब ‘चिगुन’ स्वयं ‘चि’ से व्युत्पन्न है जिसका रिश्ता ‘किम’ से है। शब्दों का सफ़र में पहले बताया जा चुका है कि पुरानी फ़ारसी-तुर्की में ‘किम्’ का एक रूप ‘चिम्’ होता हुआ ‘चि’ में तब्दील हुआ है।
तो चूँकि में क्योंकि वाले आशय समाहित है अर्थात ‘इसलिए’, ‘जैसे कि’, ‘कारण कि’ वगैरह आशय इससे स्पष्ट होते हैं। फ़ारसी में चूँ-चपड़ की जगह ‘चूँ-चिरा’ या ‘चूँ ओ चिरा’ पद प्रचलित है जिसका आशय है “कब, क्यों कहाँ”. इससे जो मुहावरा बनता है “चूँ-चिरा न करना” यानी बात वही ज्यादा सवाल न पूछो। हिन्दी ने इससे ही चूँ-चपड़ बना लिया। पुरानी हिन्दी में यह बतौर “चूँचरा” मौजूद है जिसका अर्थ है प्रतिरोध, विरोध, प्रतिवाद आदि।
निष्कर्ष- पत्रकारों को हमेशा चूँ-चपड़ करते रहना चाहिए यानी 'ककारषष्ठी' मन्त्र का जाप जारी रहे।
ये सफर आपको कैसा लगा ? पसंद आया हो तो यहां क्लिक करें
|